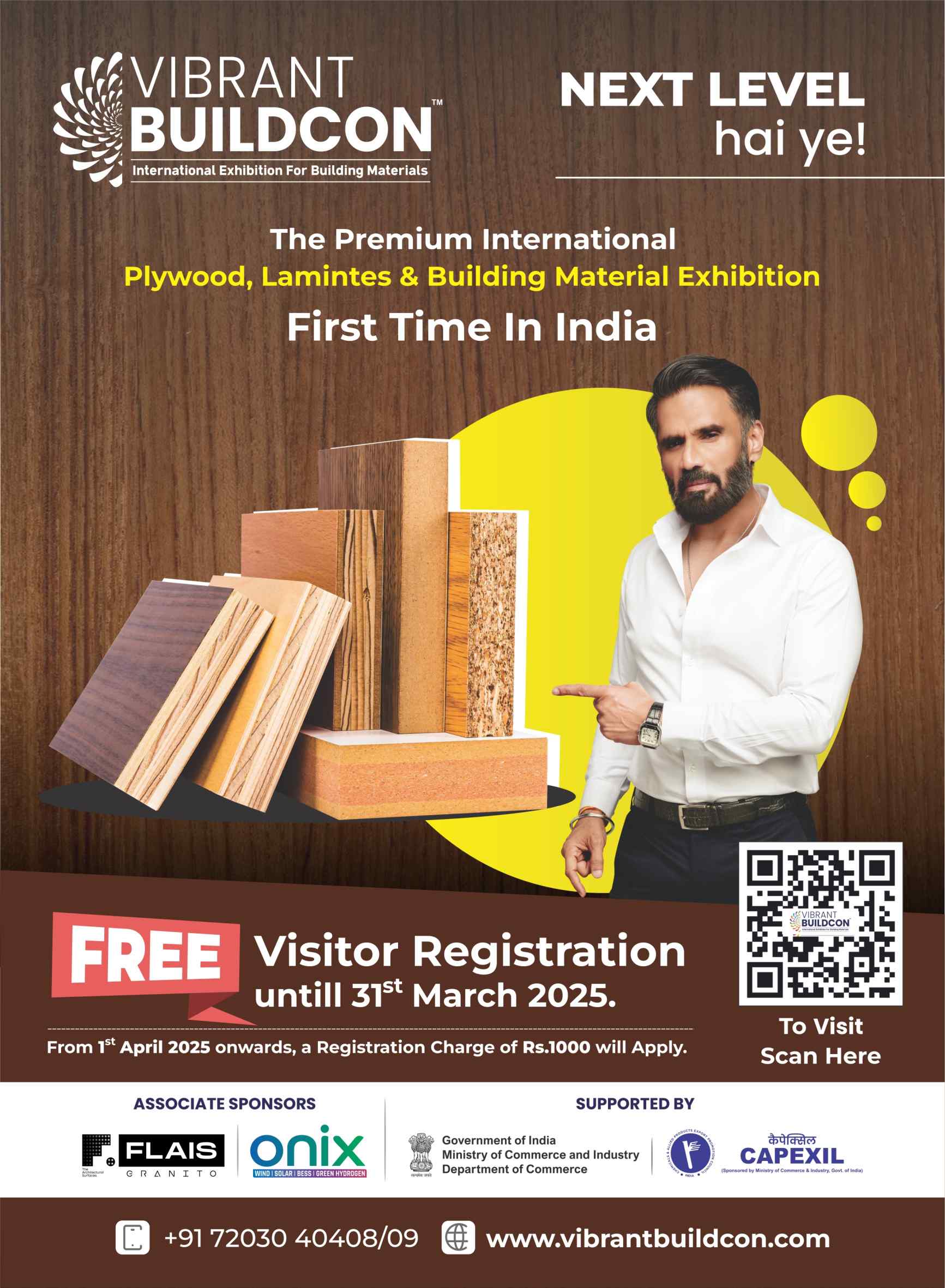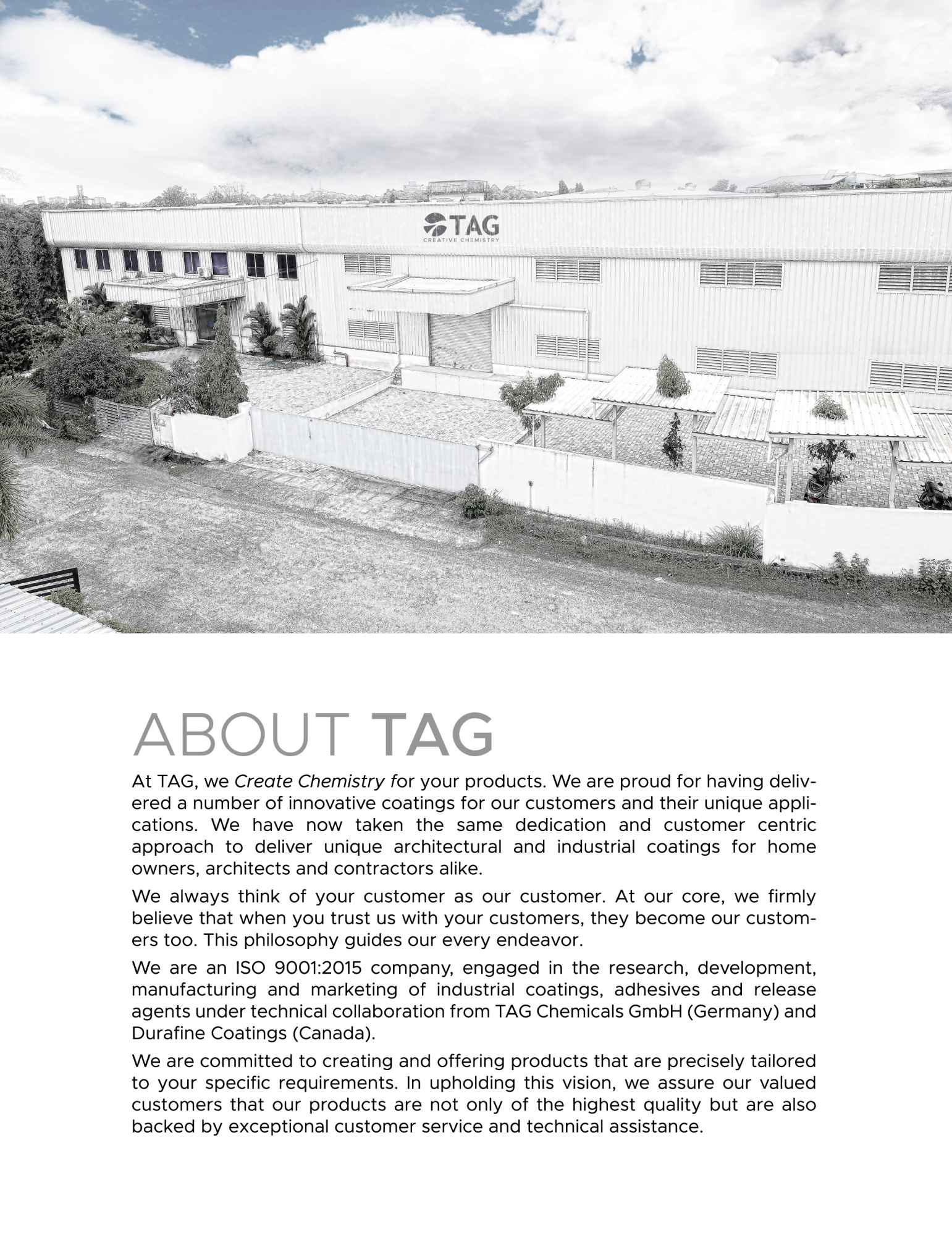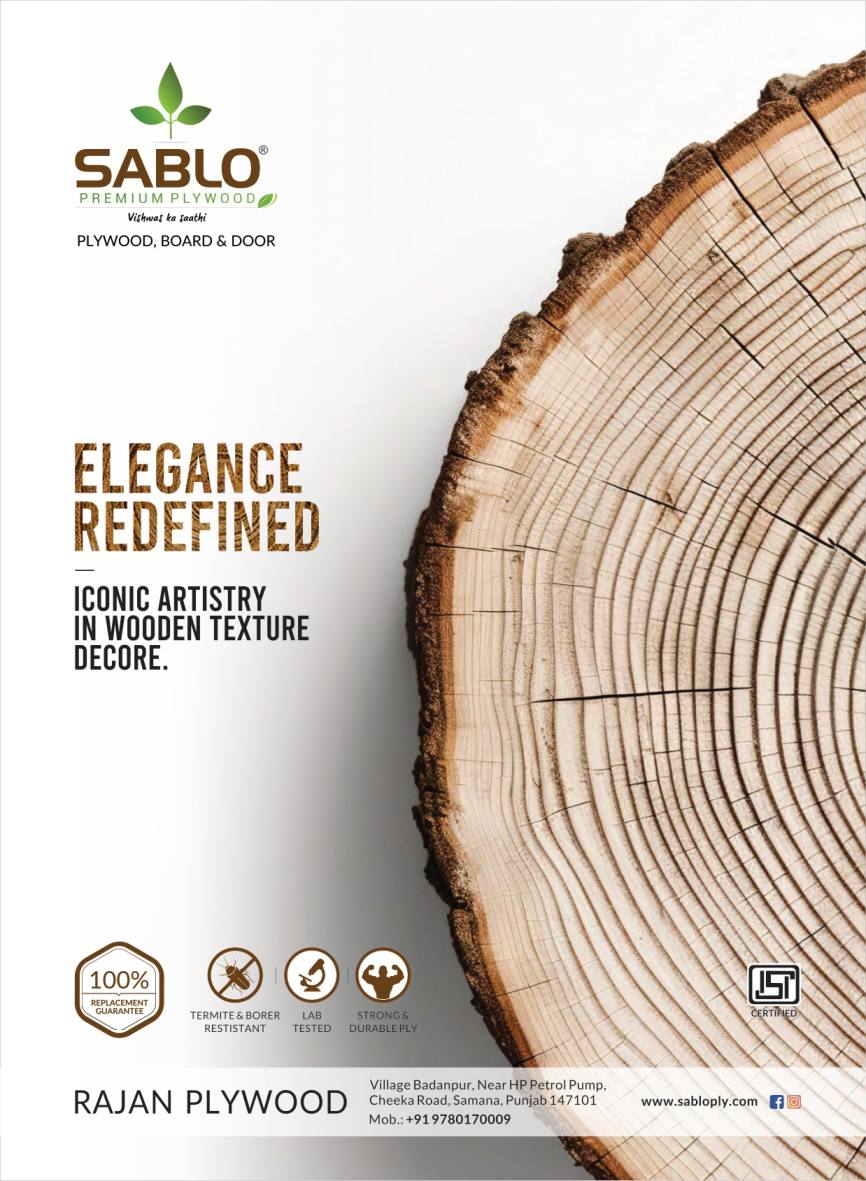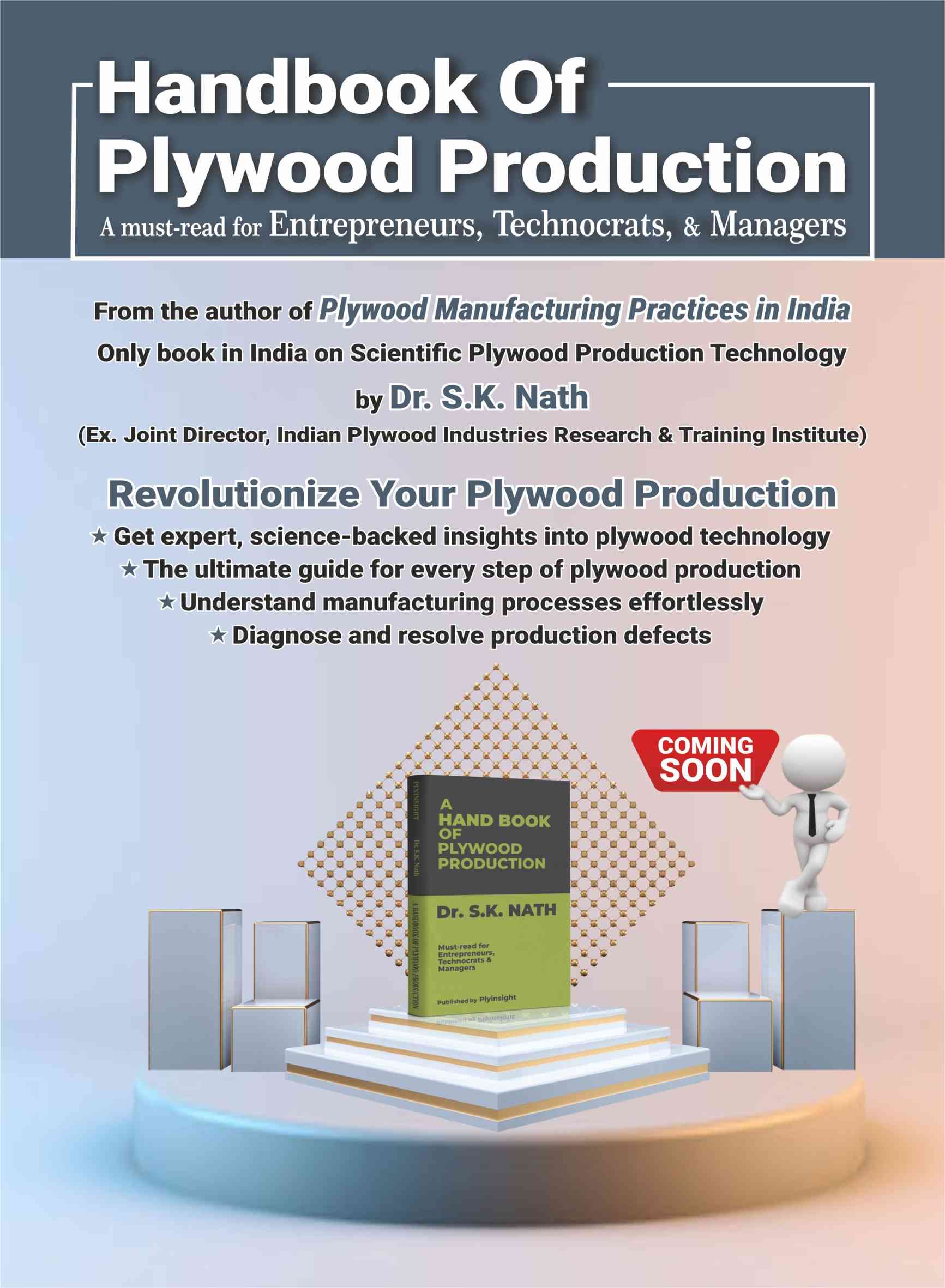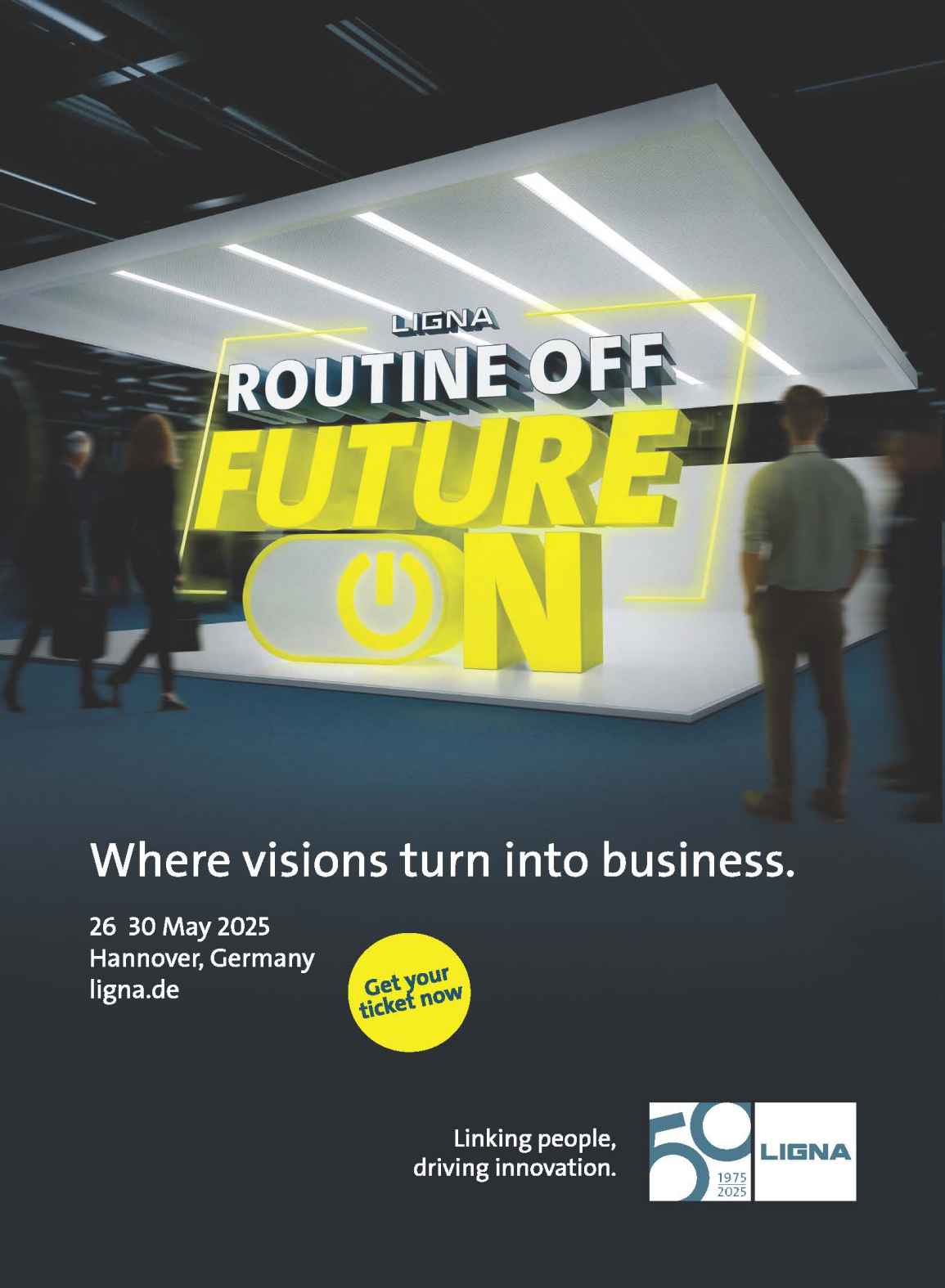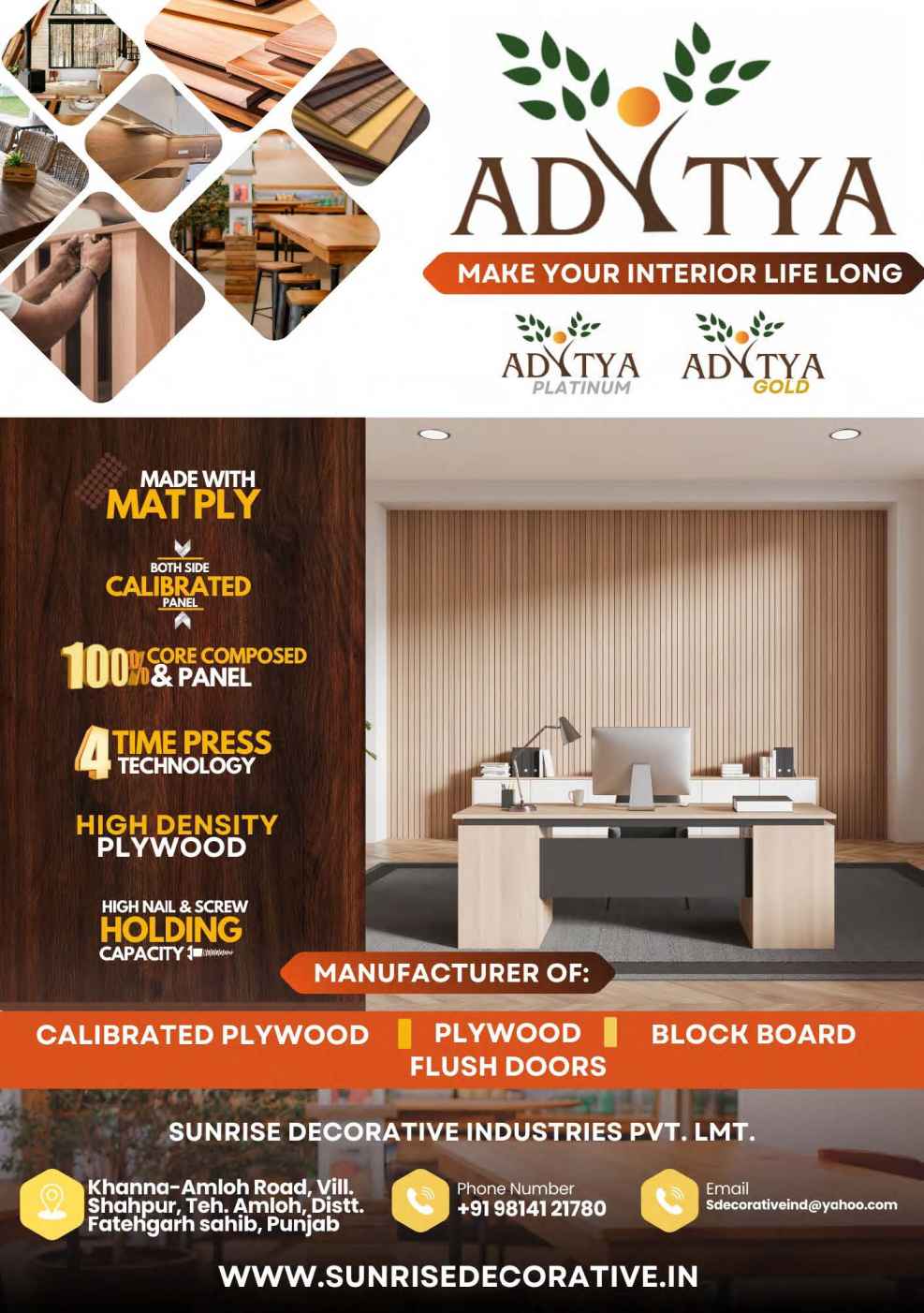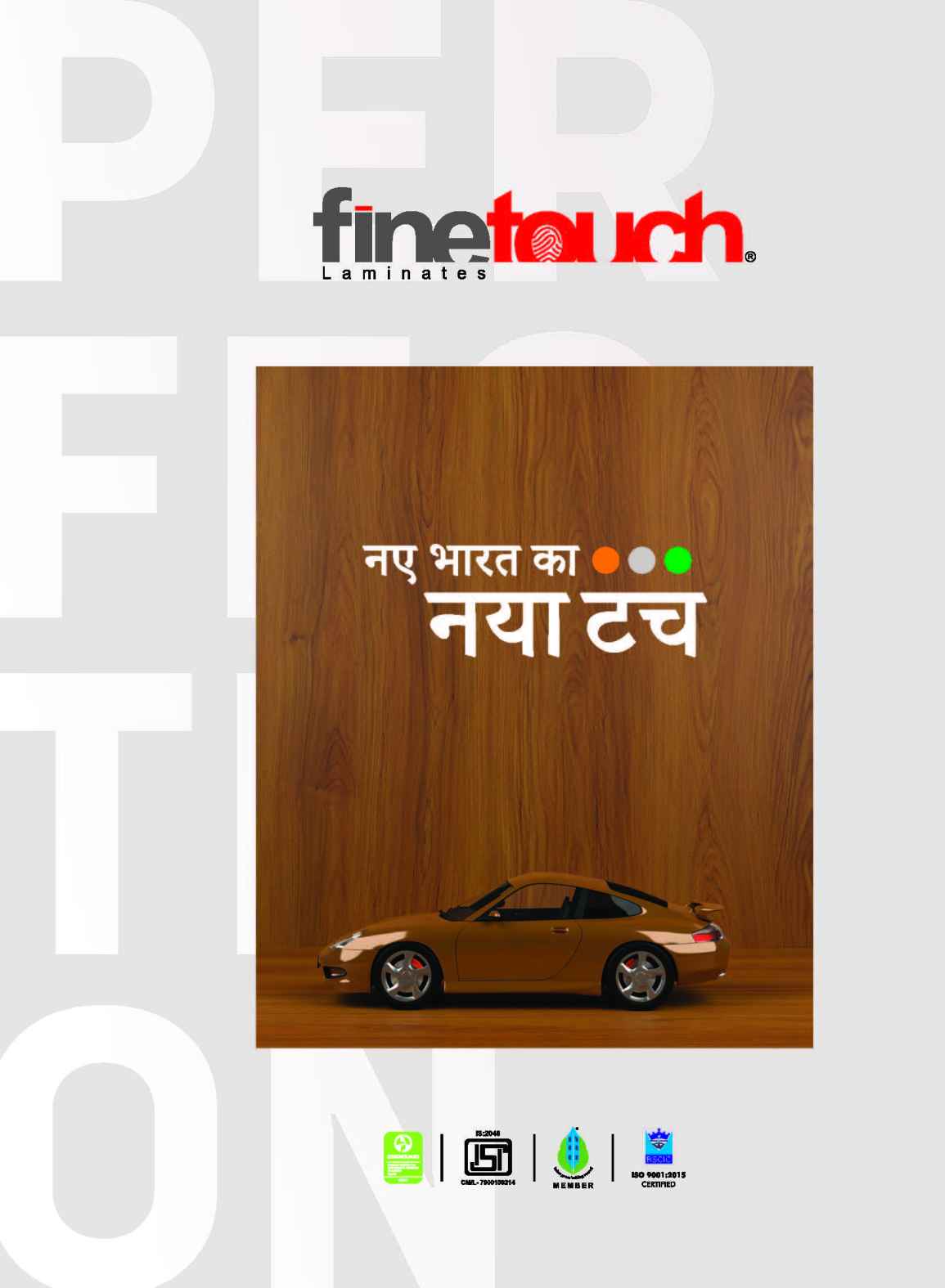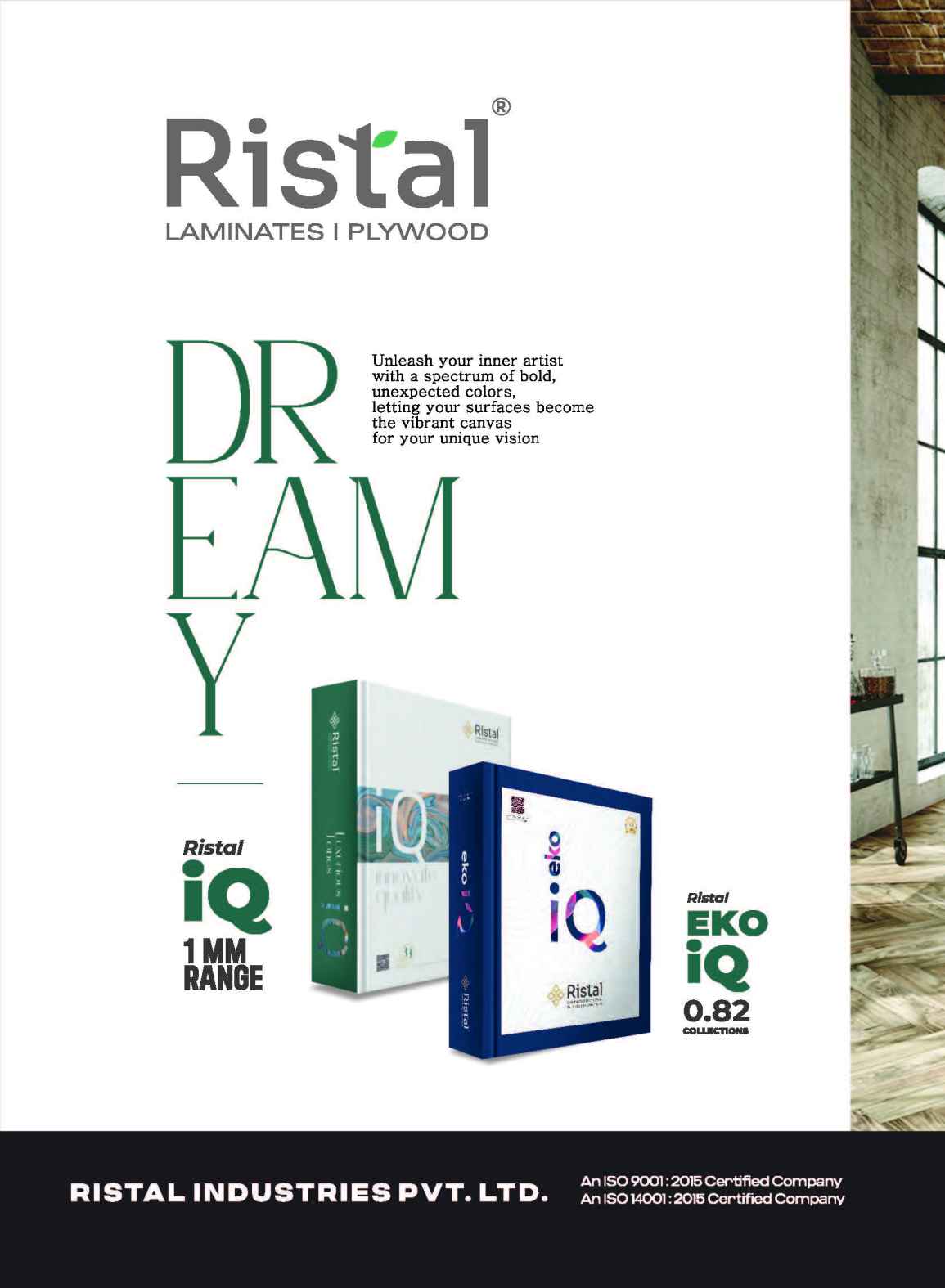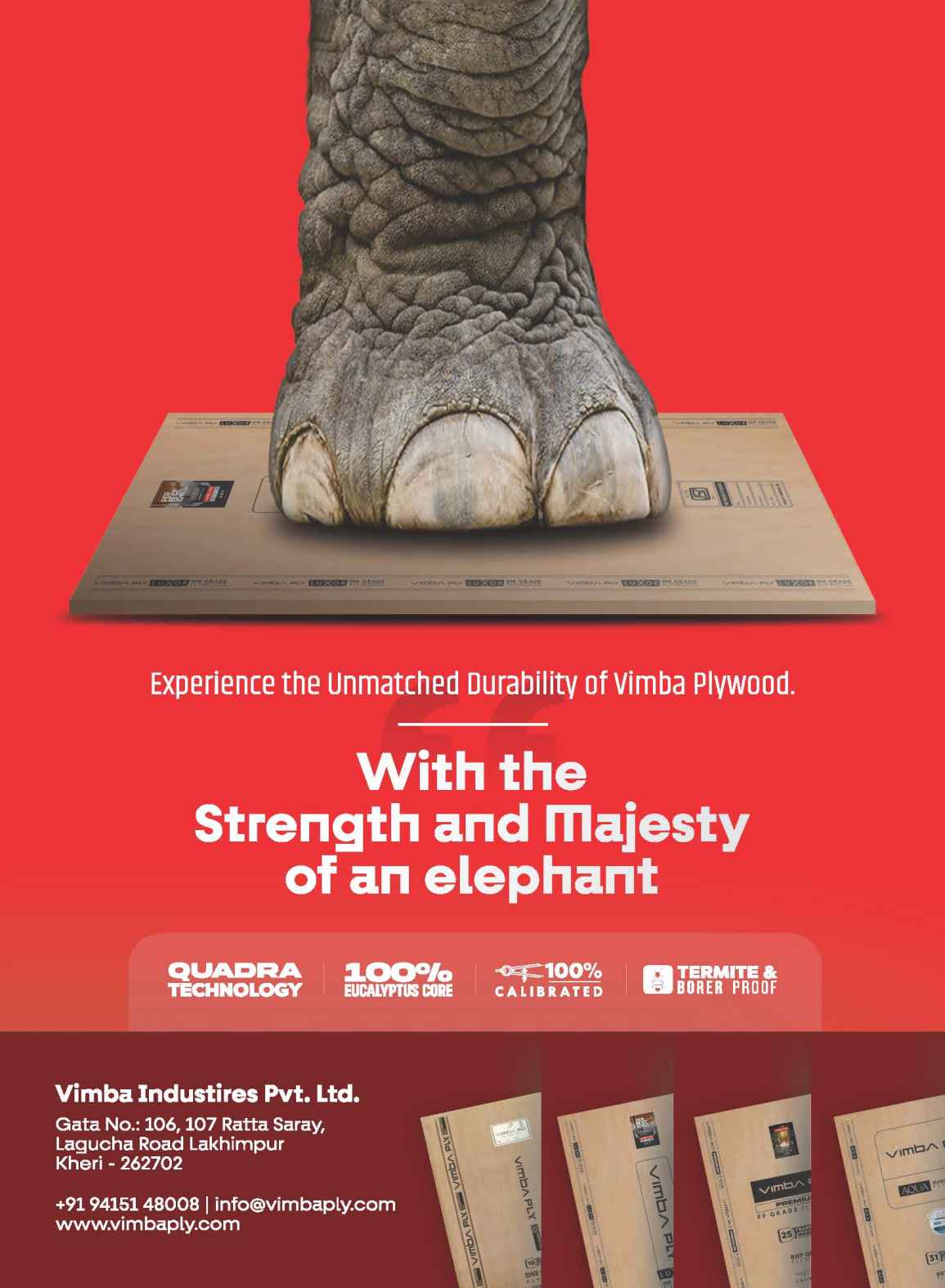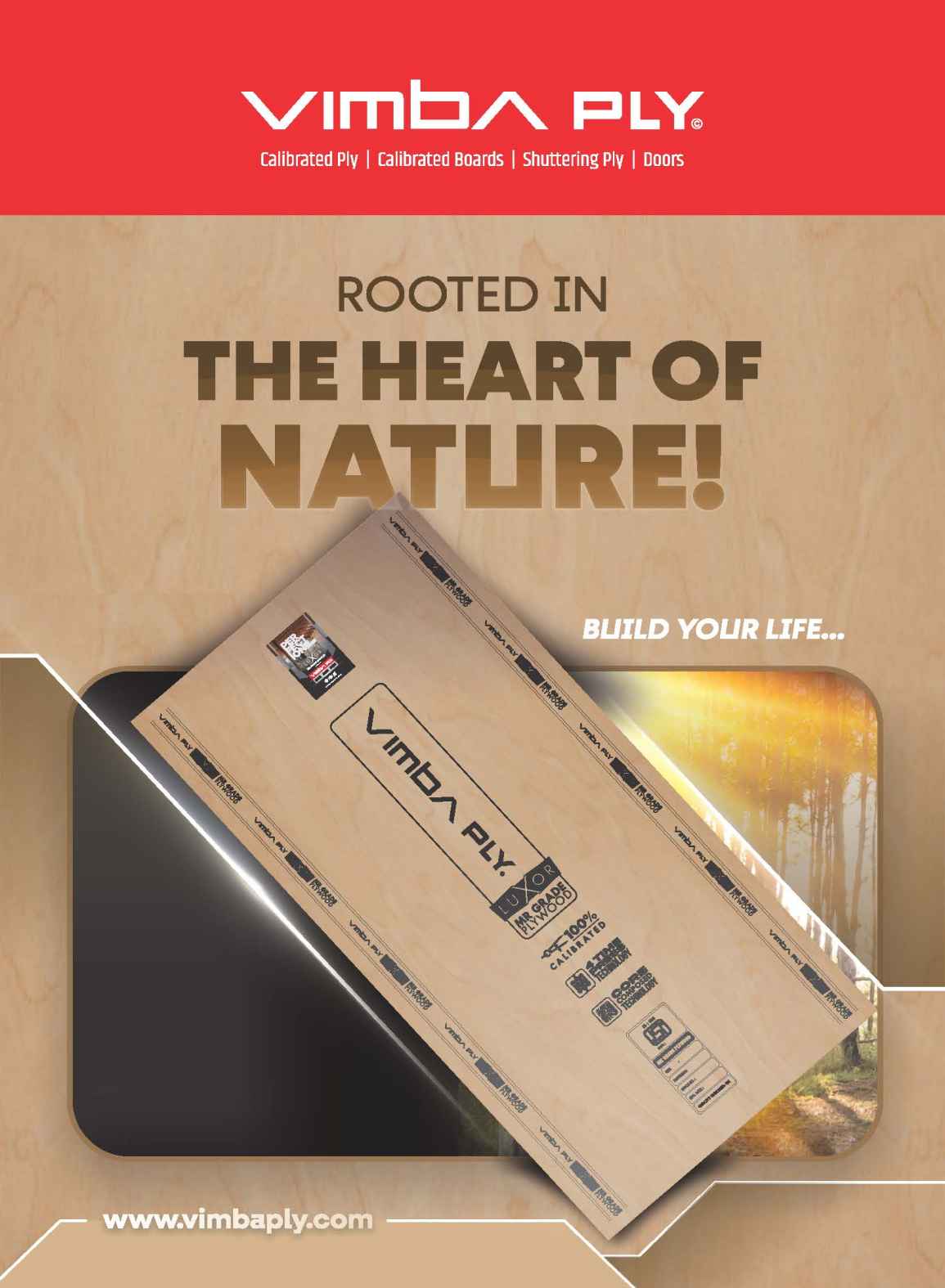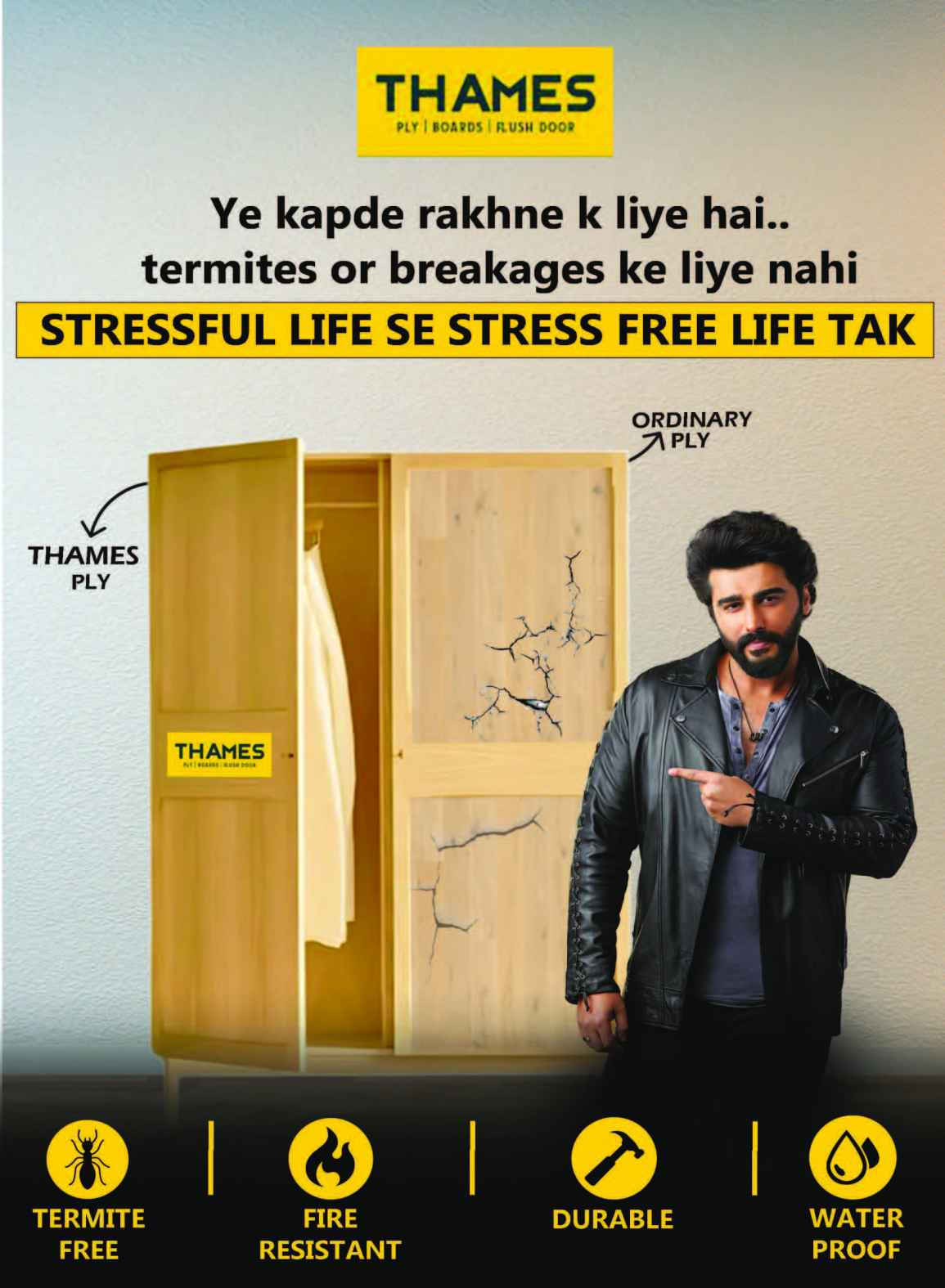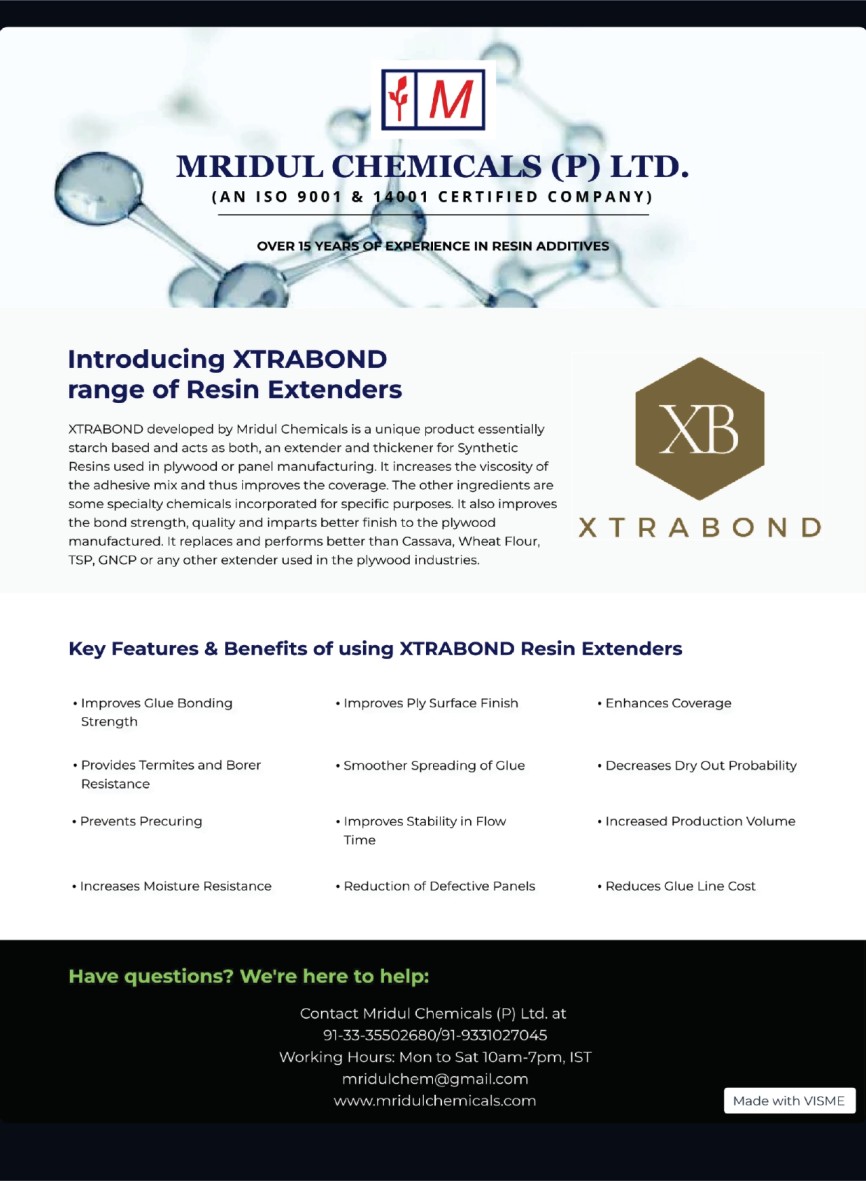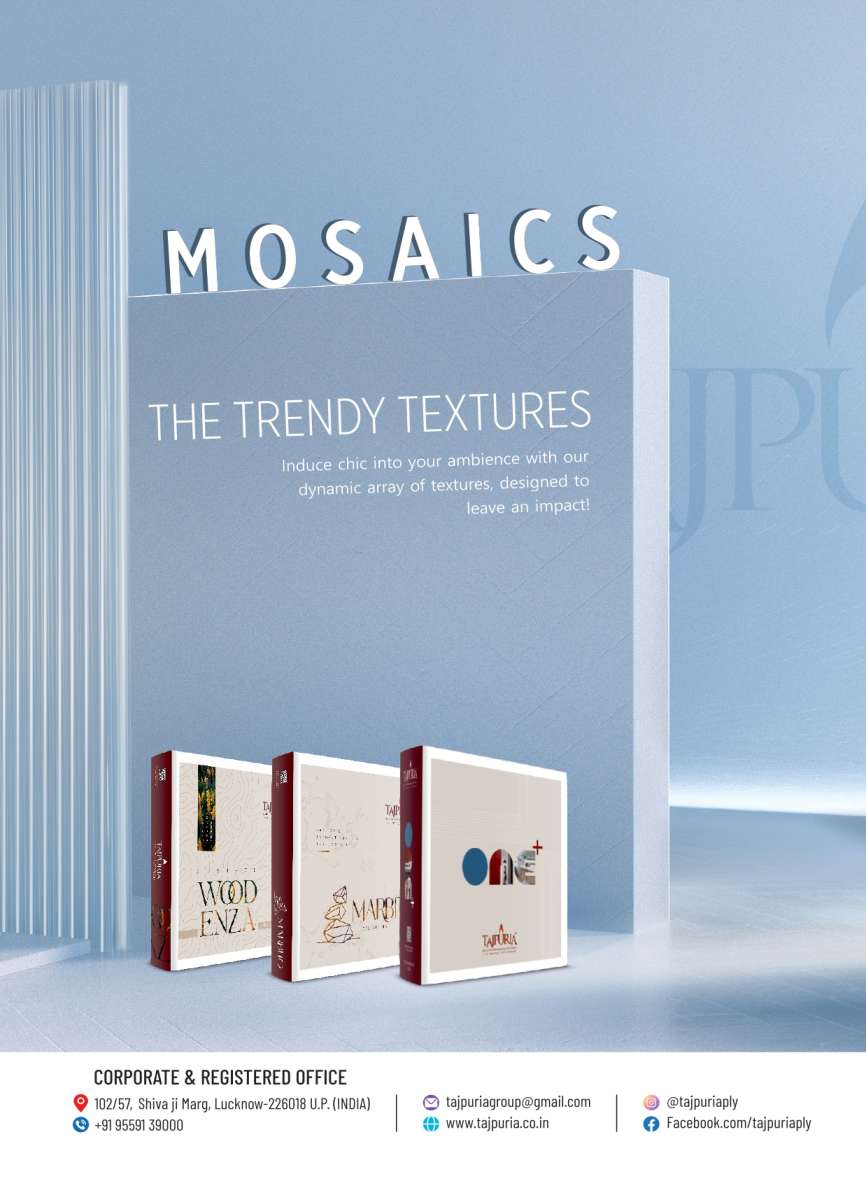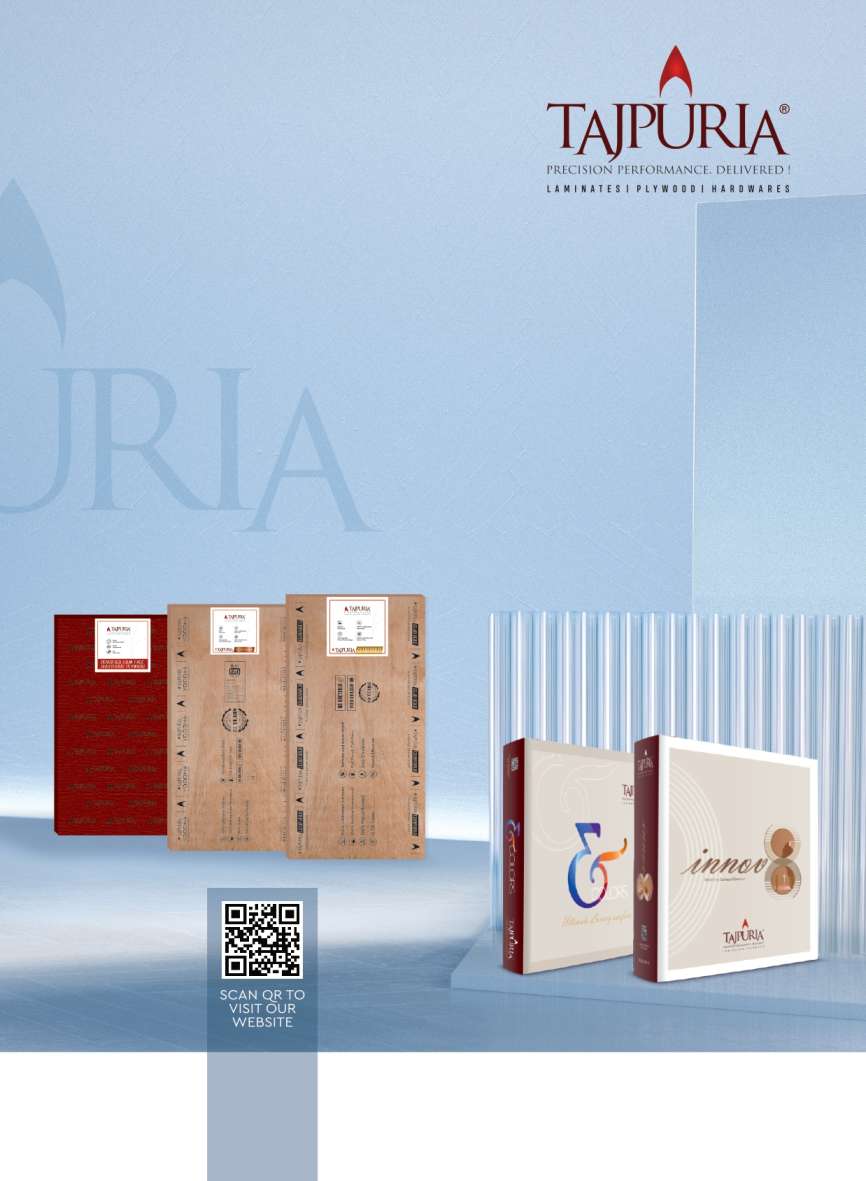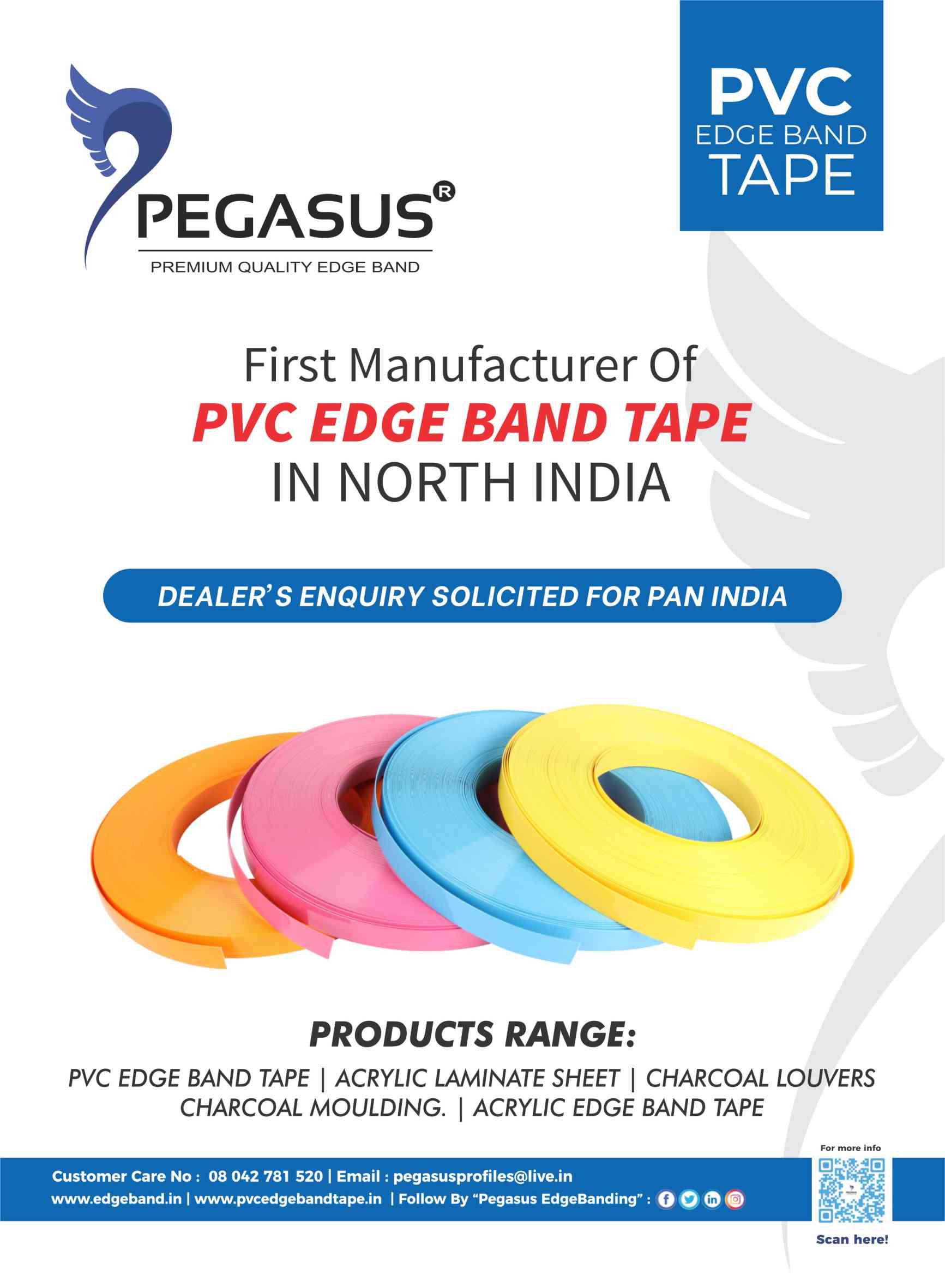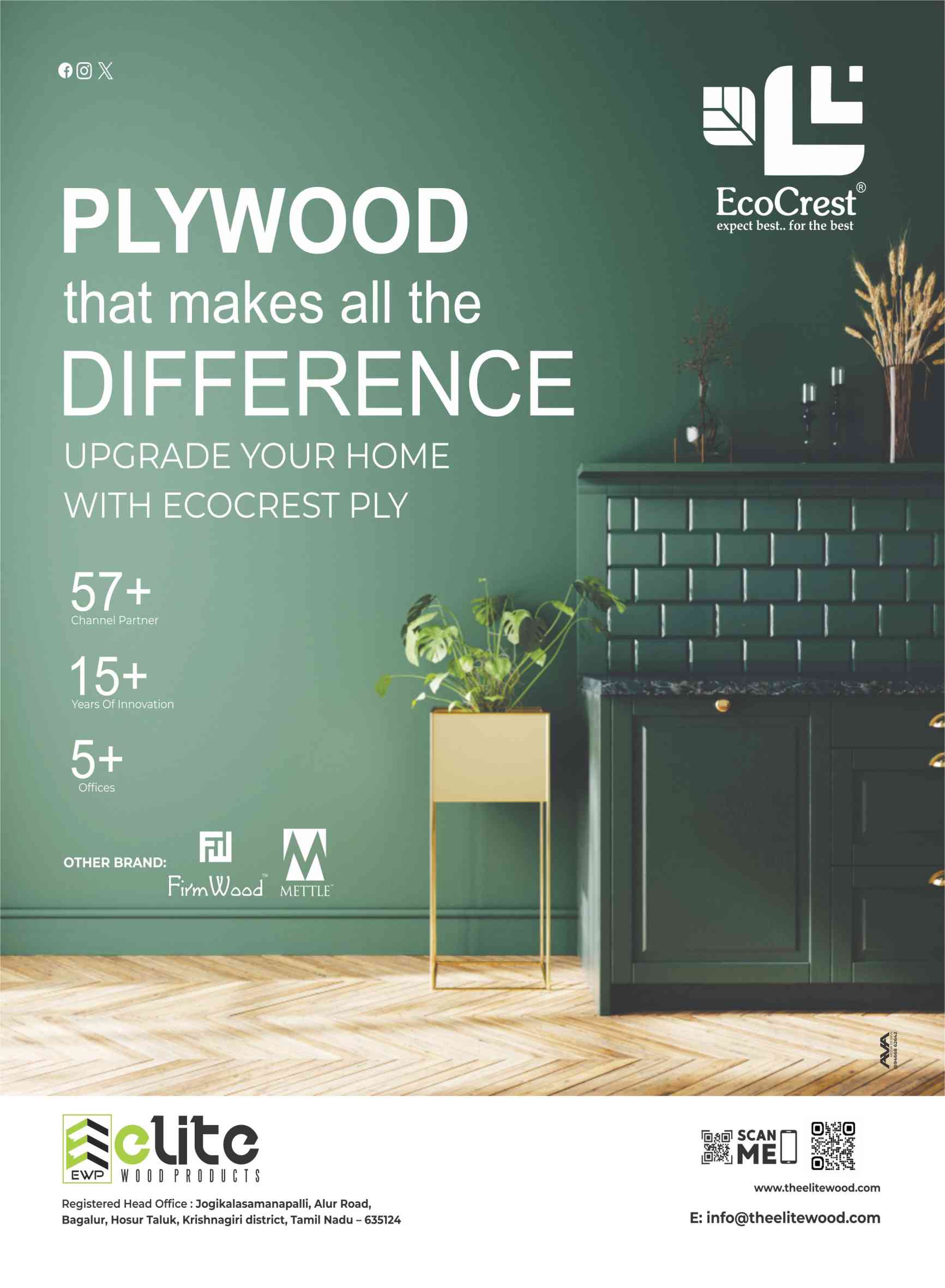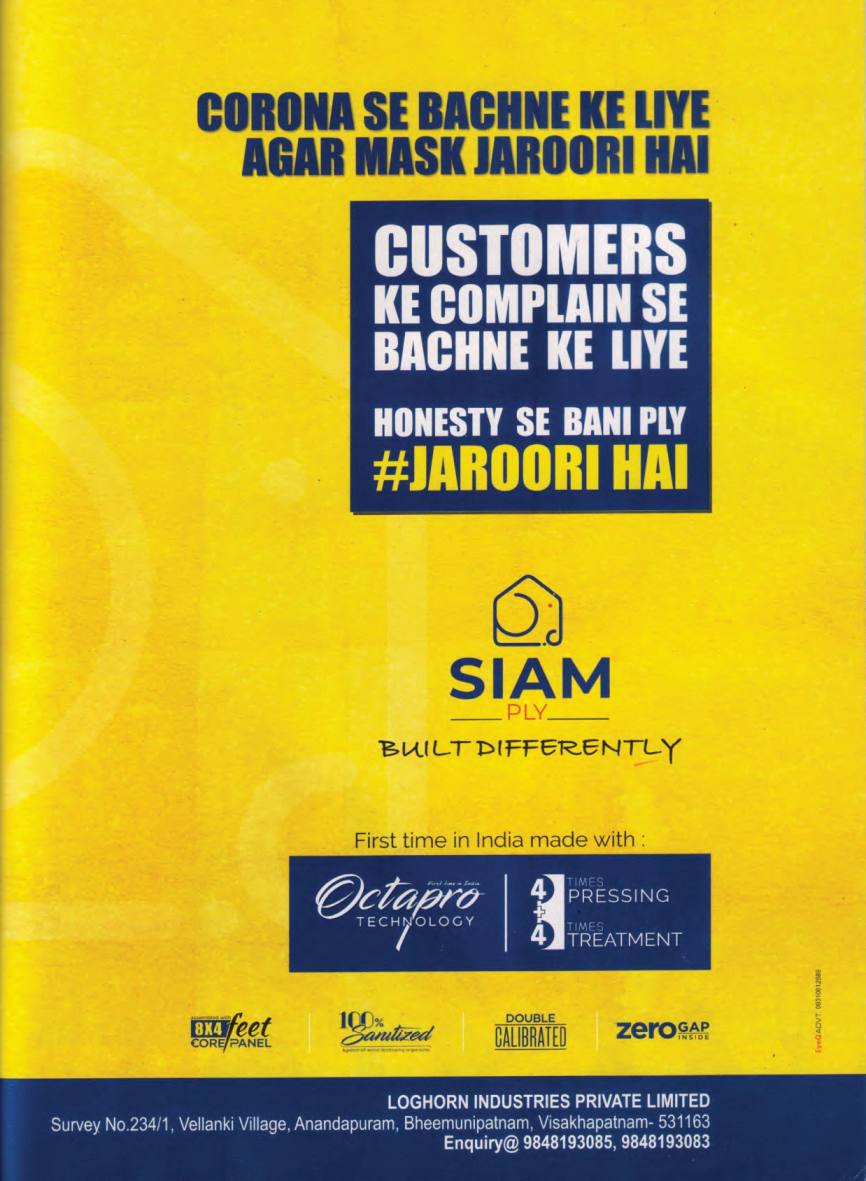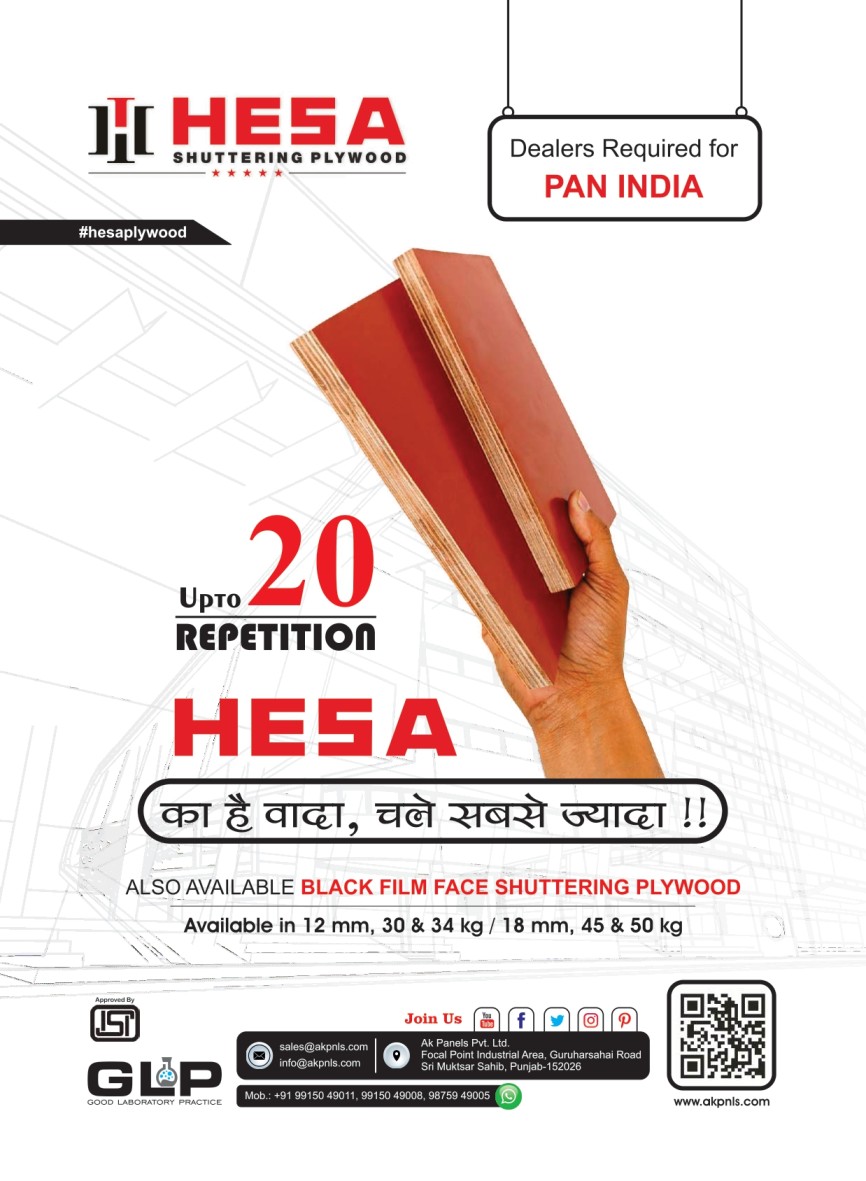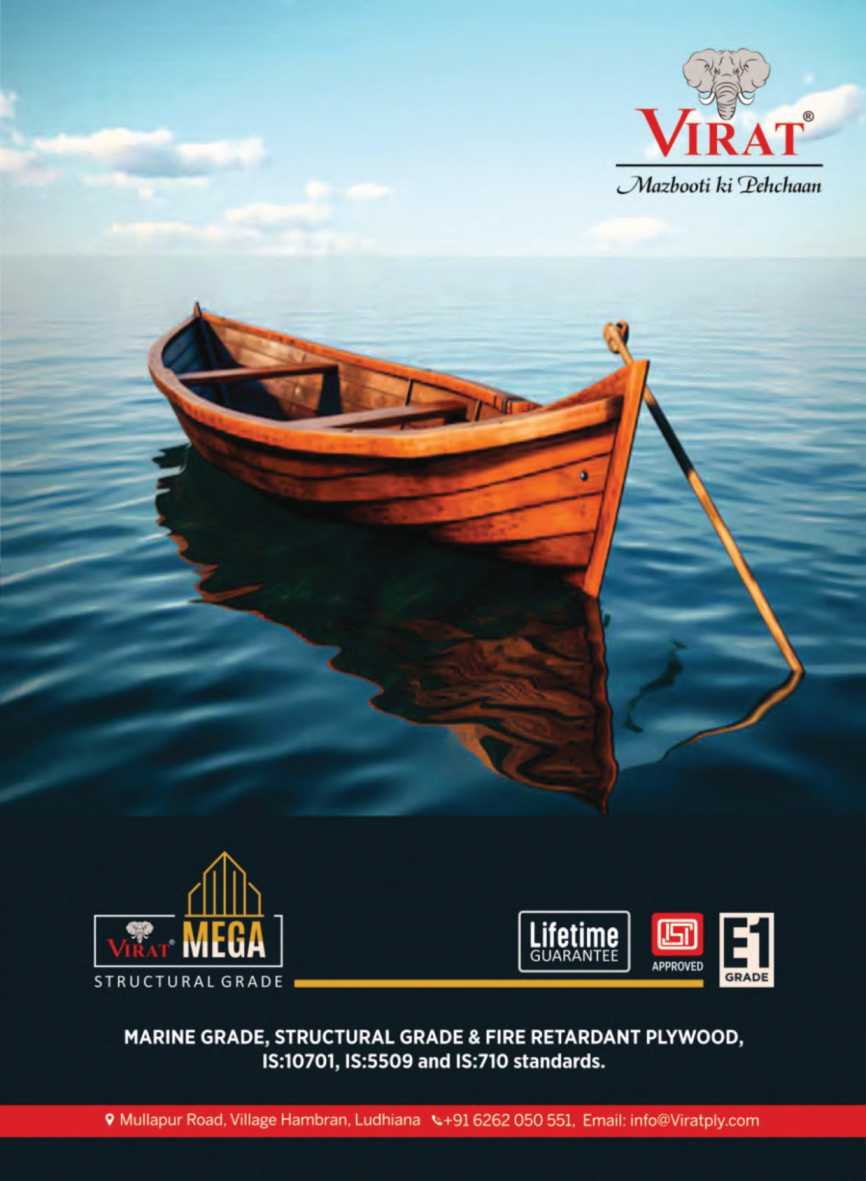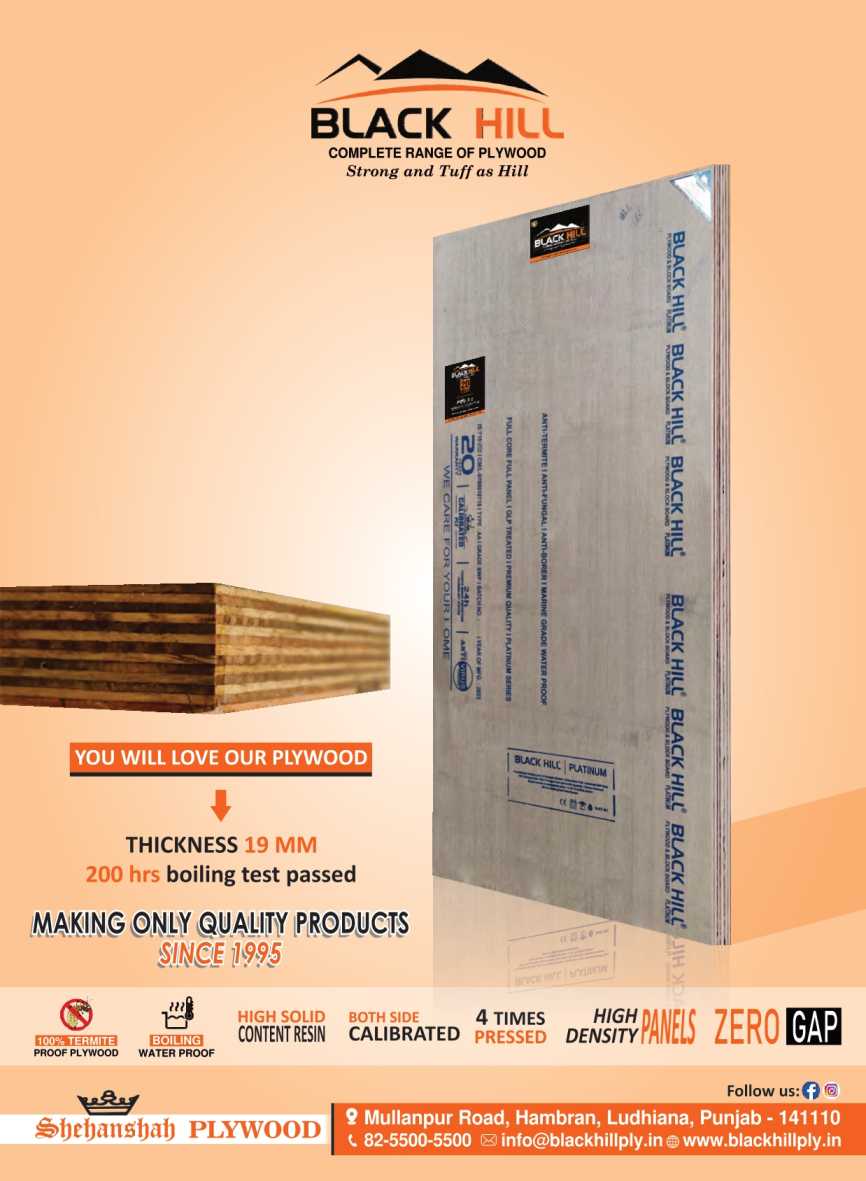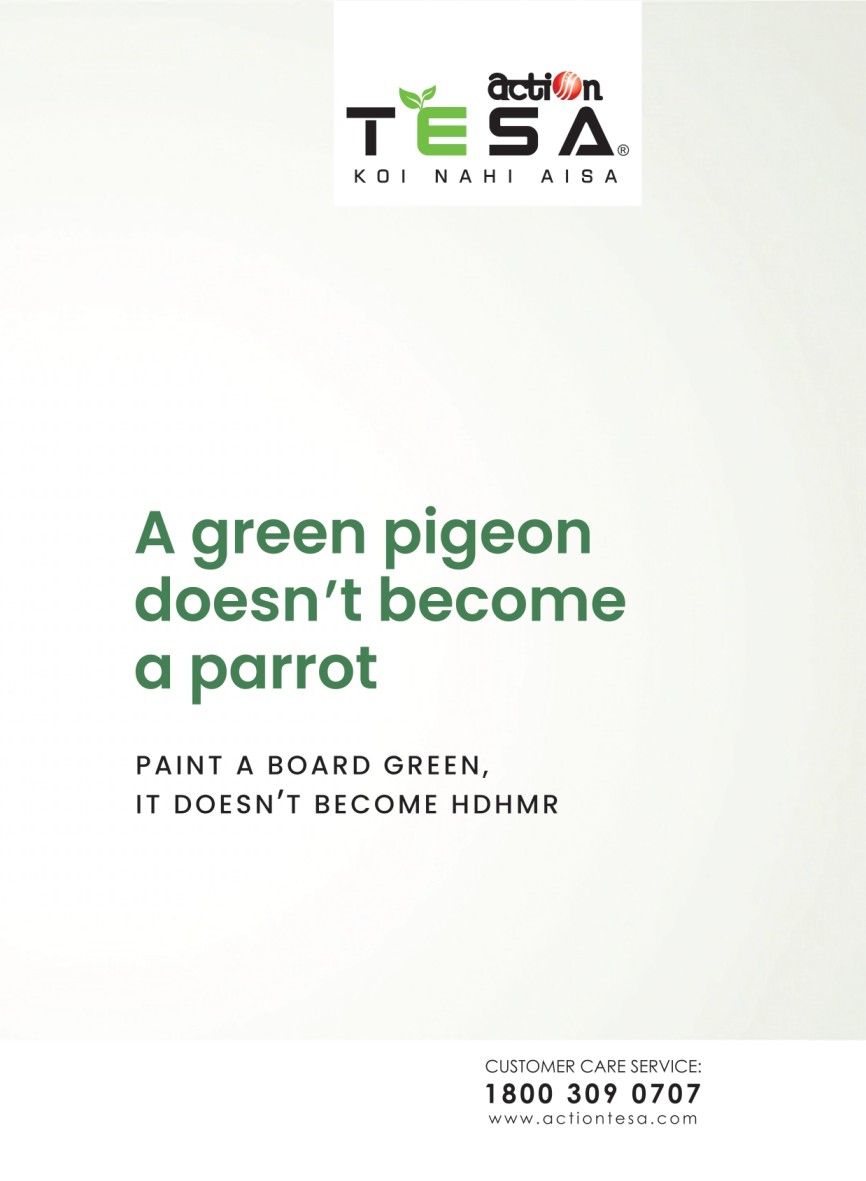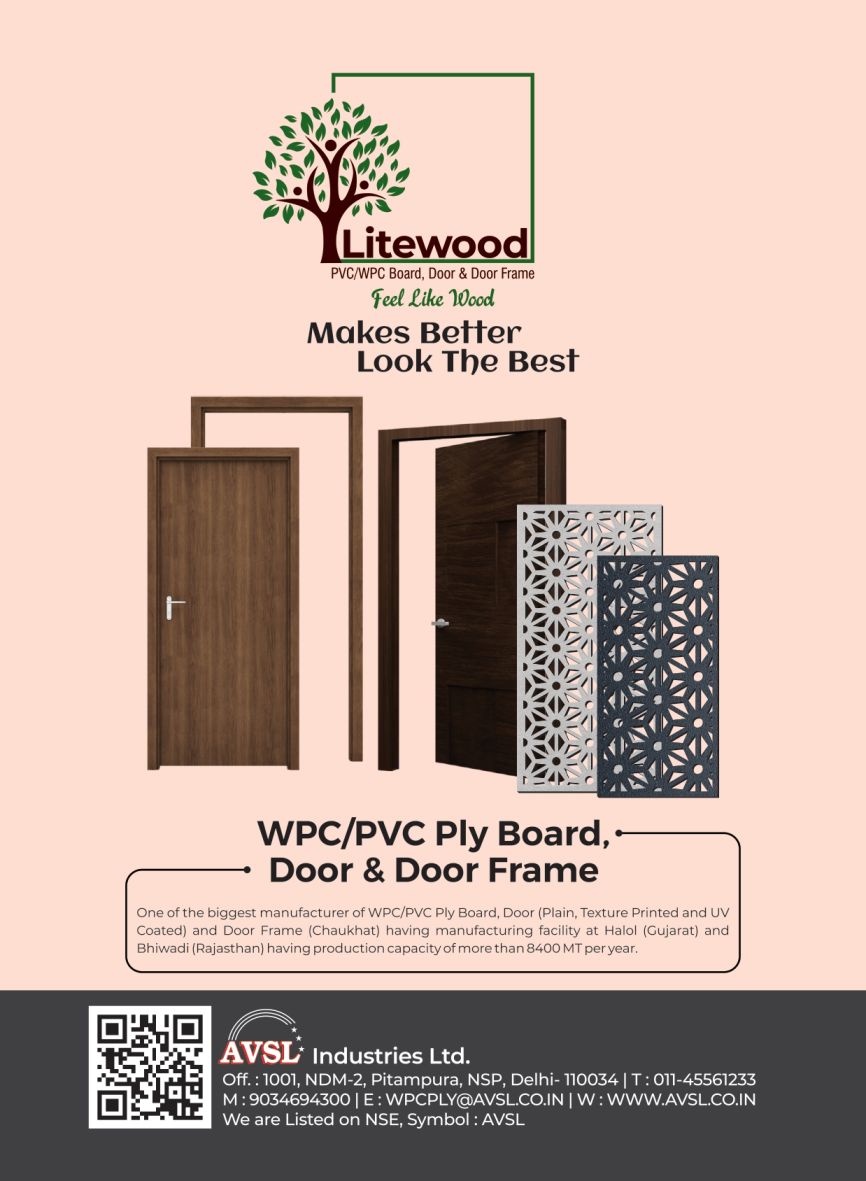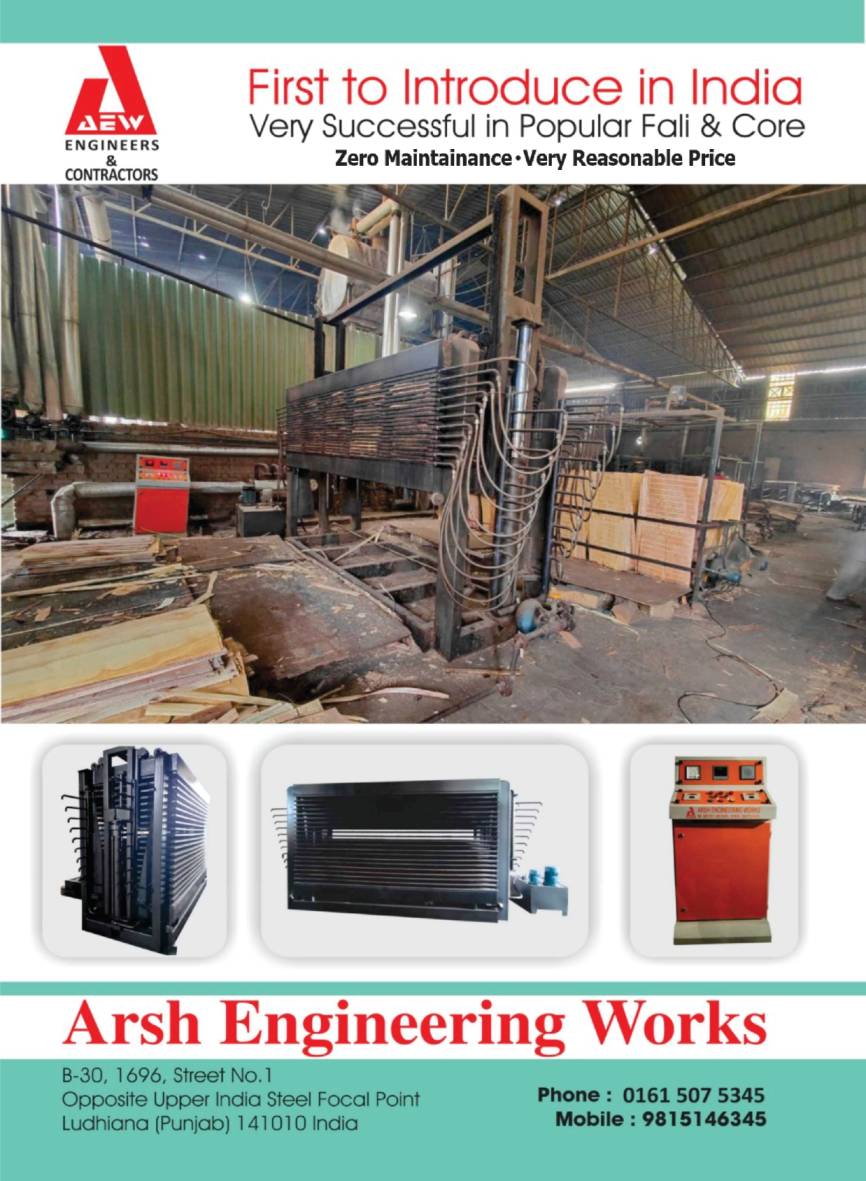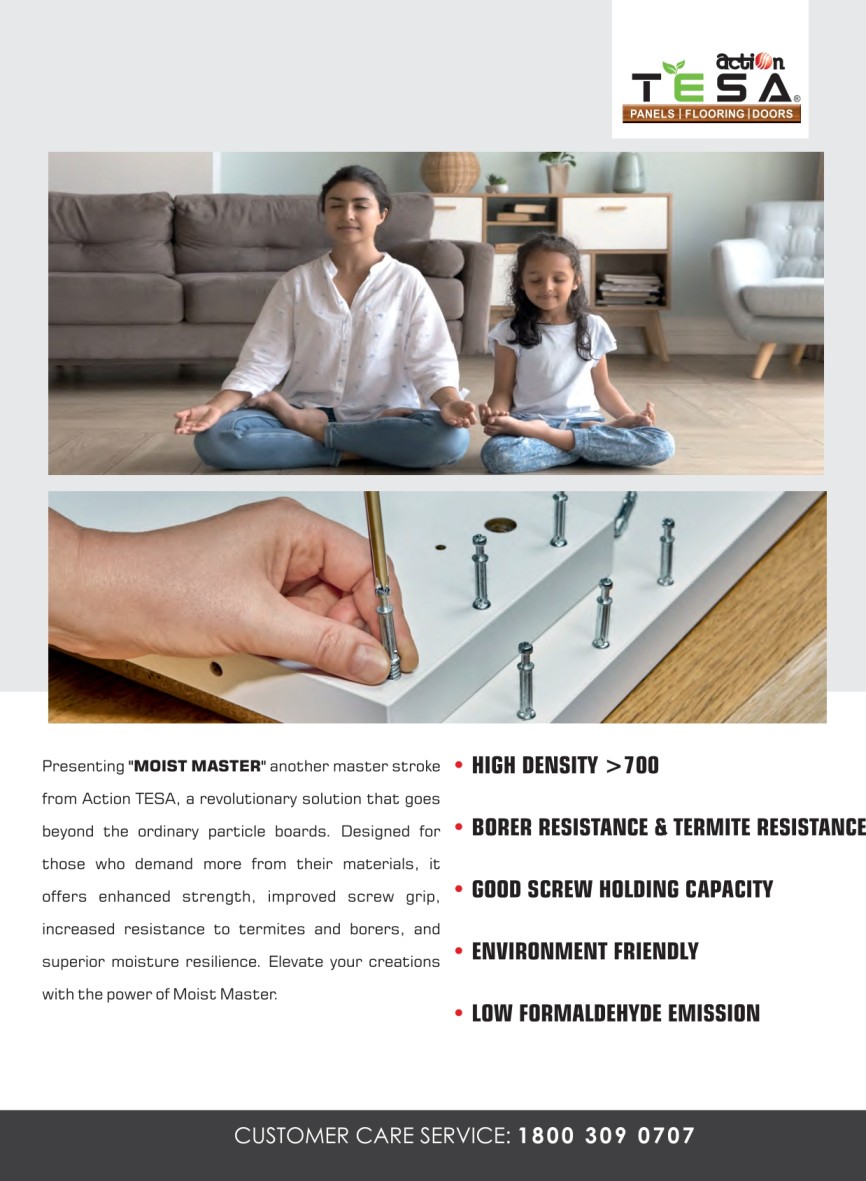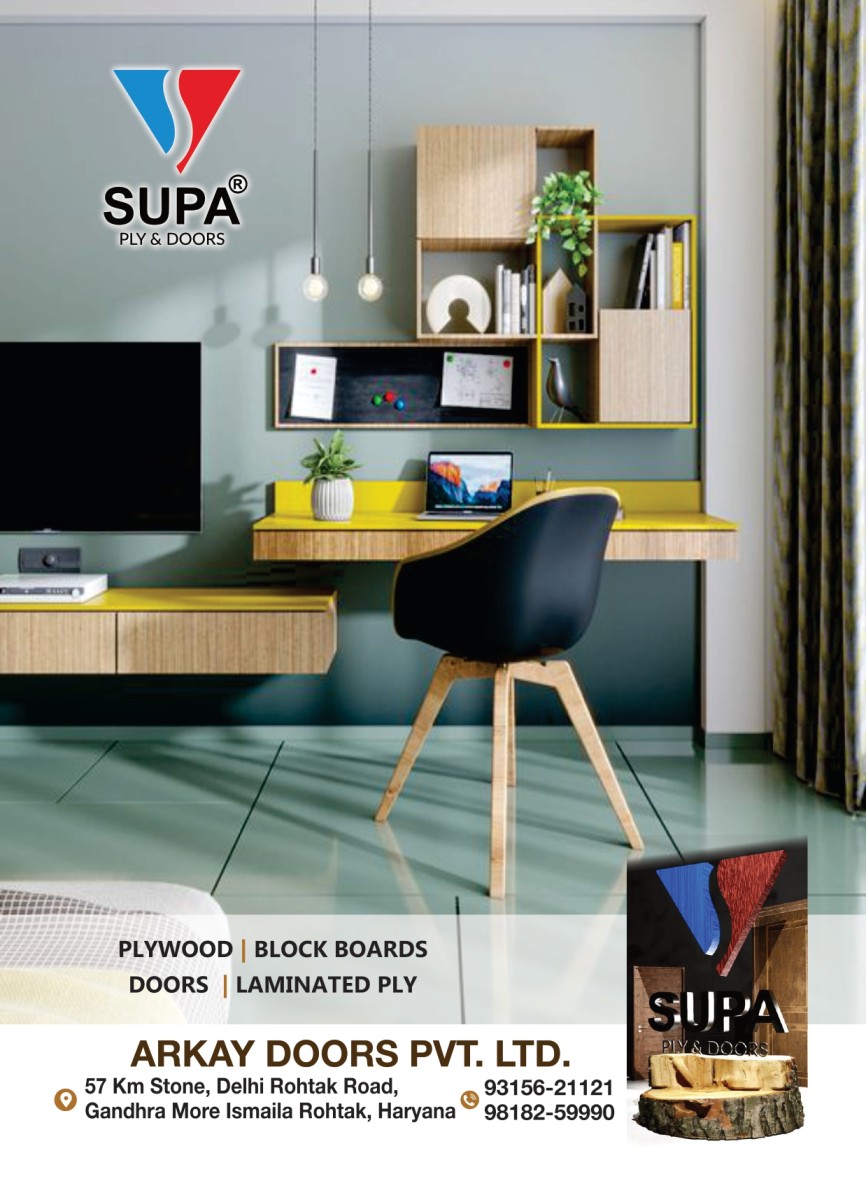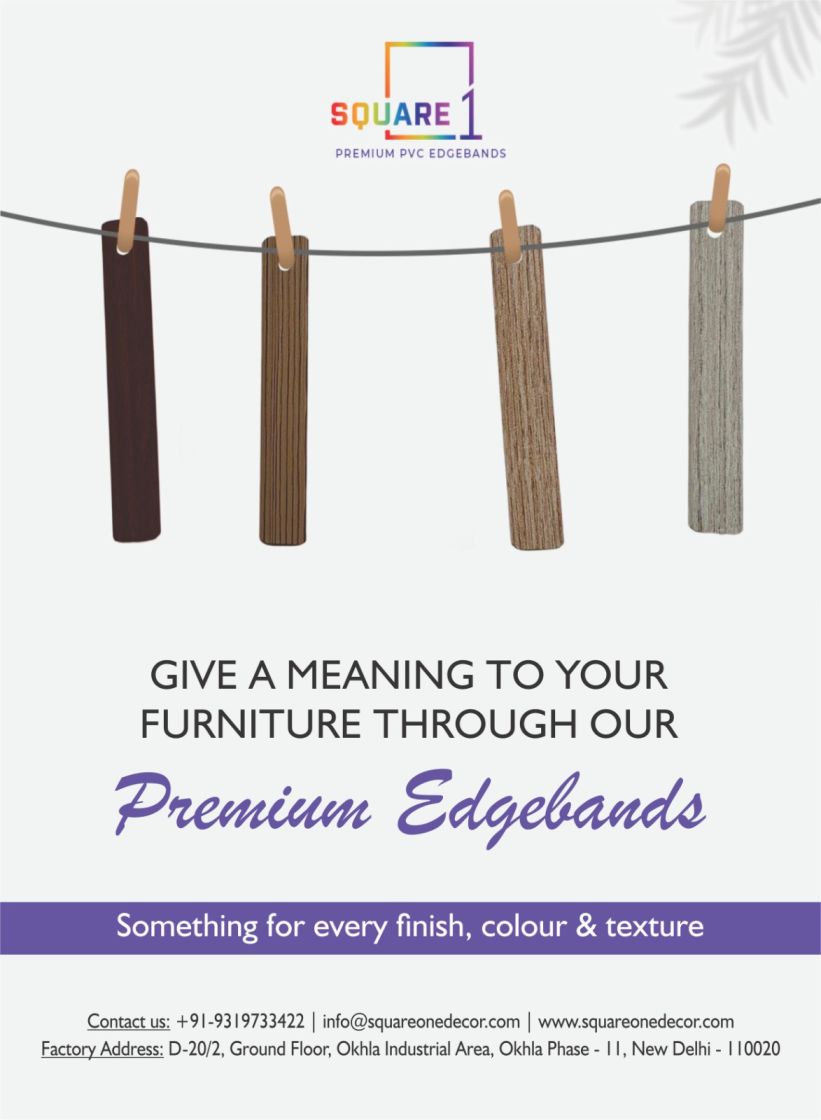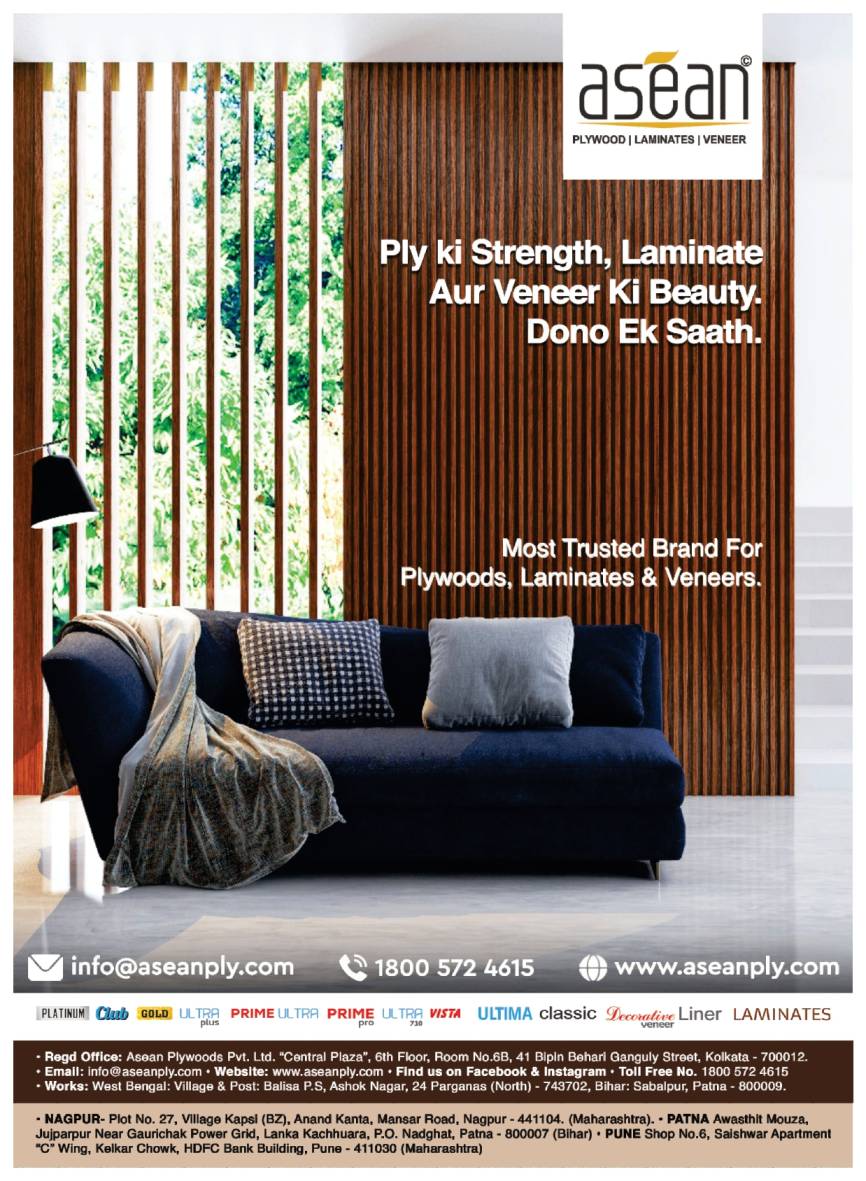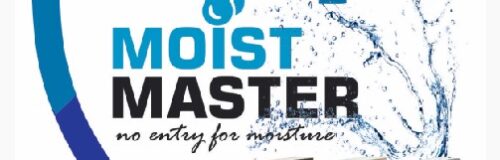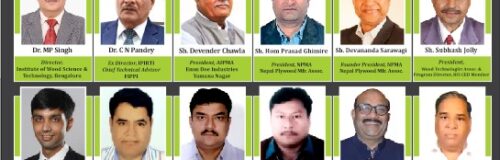निर्यात की महत्वाकांक्षा के लिए उत्पादन में निवेष
- फ़रवरी 7, 2025
- 0
अगर उद्योग, आर्थिक नीति तथा राजनीति मददगार रहीं तो अगली चौथाई सदी भारत की हो सकती है।
1991 से 1993 तक जो सुधार किए गए थे उनकी बदौलत वृद्धि को गति मिली। औद्यौगिक लाइसेंसिग को समाप्त करने का अर्थ था सरकार ने यह तय करना बंद कर दिया कि किन क्षेत्रों में उद्योग को निवेश करना चाहिए और किन में नहीं।
अर्थव्यवस्था को कम शुल्क वाले आयात के लिए खोला गया तो भारतीय कंपपियों को सर्वश्रेष्ठ के साथ मुकाबला करना पड़ा। स्वतंत्र संस्थाओं को काम करने की इजाजत दी गई और ऐसे नियम बनाए गए जिनके तहत सभी काम कर सकें। 1991 से 2018 के बीच कारर्पोरेट और व्यक्तिगत आय कर घटाए गए, जिससे उद्यमी कानूनी तरीके से धन जुटा सके।
2017 के वस्तु एवं सेवा कर सुधारों से देश भर में वस्तुओं का अबाध आवागमन संभव हुआ। सरकार ने विभिन्न उद्योगों से जुड़े क्षेत्रों से हाथ खींचे। इससे उद्योगों में निवेश बढ़ा।
उत्पादकता में निरंतर और दीर्घकालिक वृद्धि के लिए ढ़ाचागत बदलाव करना होगा, जिससे अर्थव्यवस्था और उत्पादक बन जाएगी। उत्पादकता बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक लोगों को काम देना होगा और उन्हें उच्च उत्पादकता वाले काम में लगाना होगा। श्रमबल में लोगों को कृषि के बजाय उद्योग तथा आधुनिक सेवाओं में रोजगार देना होगा। परंतु इसके लिए उद्योग और सेवाओं में निवेश बहुत बढ़ाना होगा ताकि लाखों लोग खेती से हटकर इन क्षेत्रों में आ सकें।
भारत के उद्योग जगत को नेतृत्व करना है तो हमें नवाचार पर गंभीर होना पड़ेगा। देश का उद्योग जगत सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का केवल 0.3 फीसदी हिस्सा आंतरिक शोध और विकास पर व्यय करता है, जबकि दुनिया भर में औसतन 1.5 फीसदी खर्च किया जाता है। हम दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और विनिर्माता हैं, लेकिन औद्यौगिक शोध और विकास में हम 21 वें स्थान पर हैं।
शोध एवं विकास के साथ हमें विश्वस्तरीय विनिर्माण और अंतरराट्रीय बिक्री पर ध्यान देने की जरूरत है। भारत को अपना ध्यान आयात कम करने के लिए उत्पादन करने की बजाय निर्यात बढ़ाने पर लगाना चाहिए। देश के उद्योग जगत की नजर में दुनिया उसका बाजार होना चाहिए।