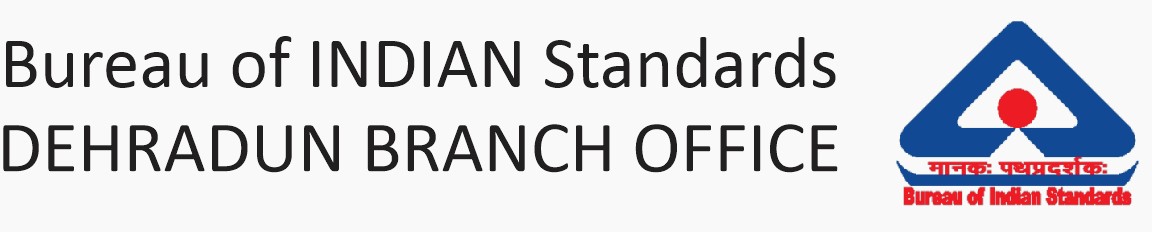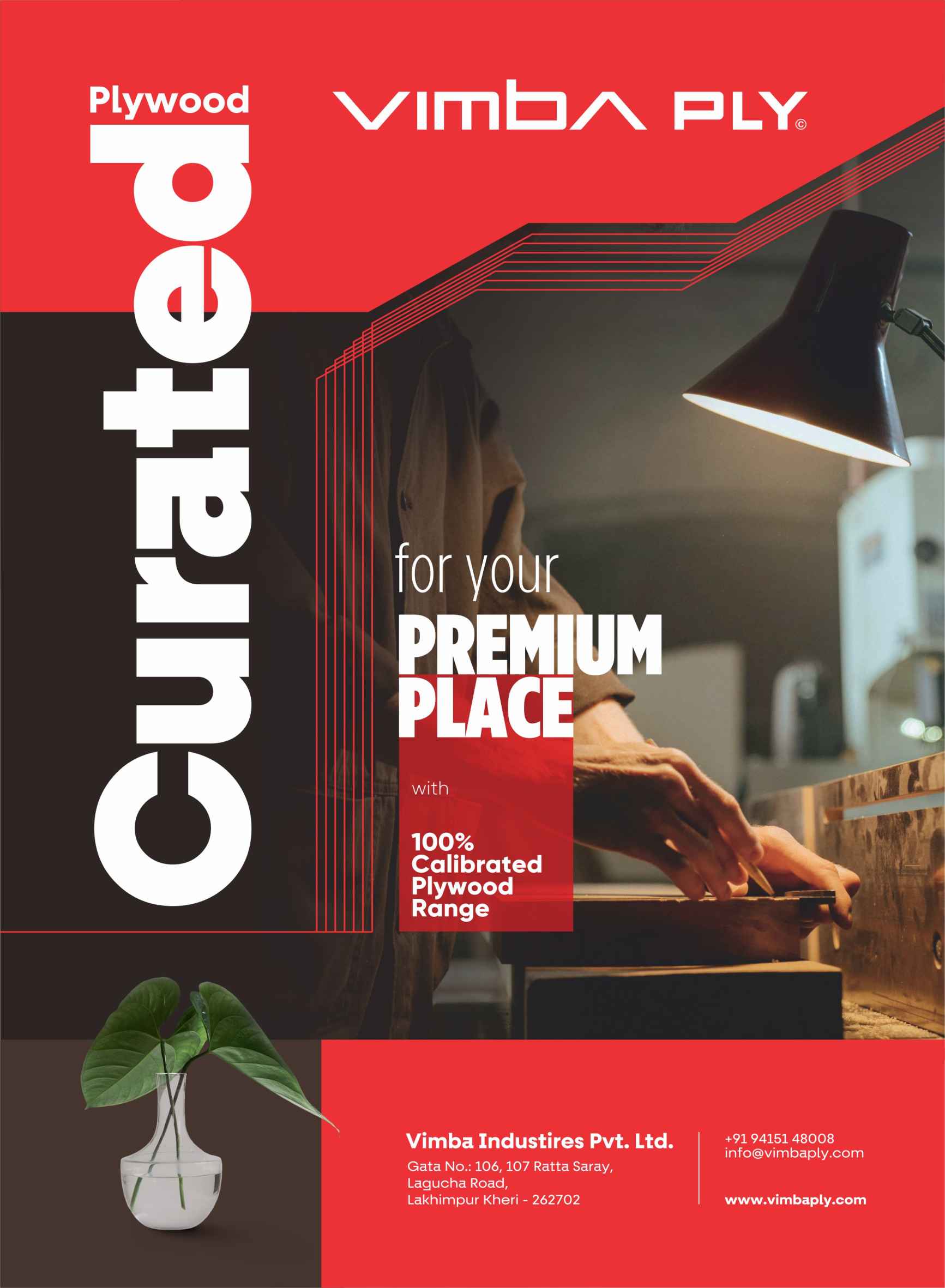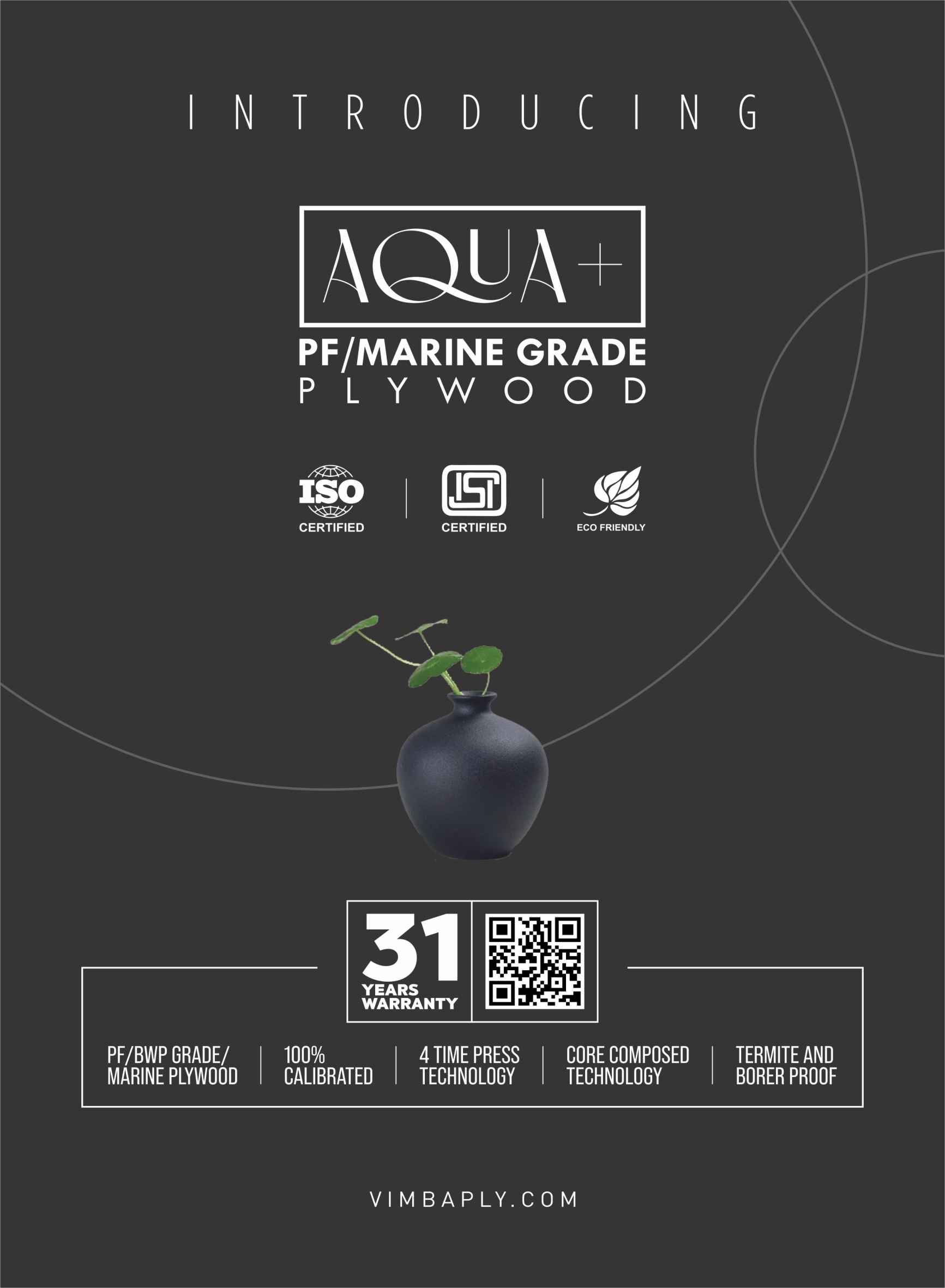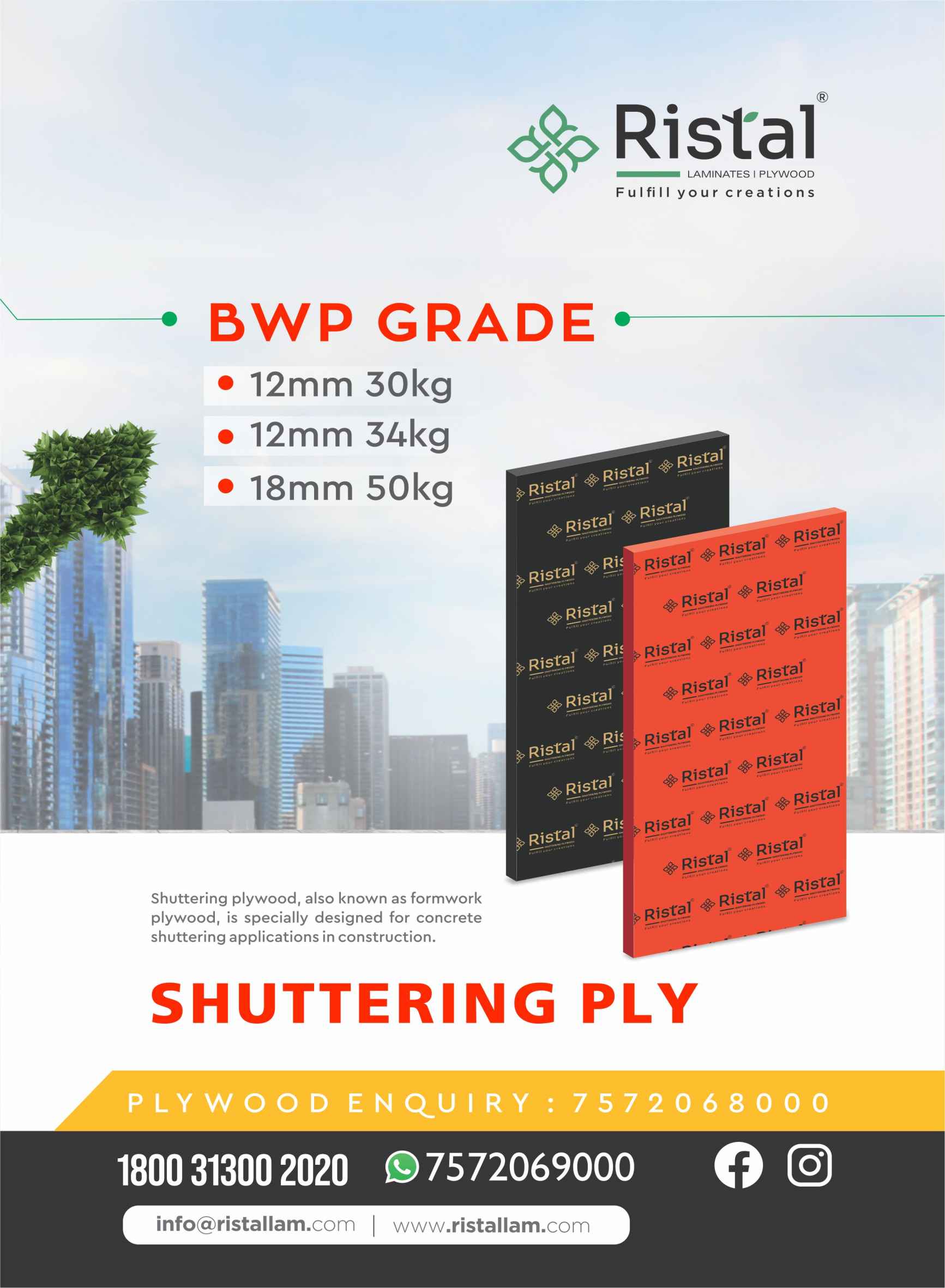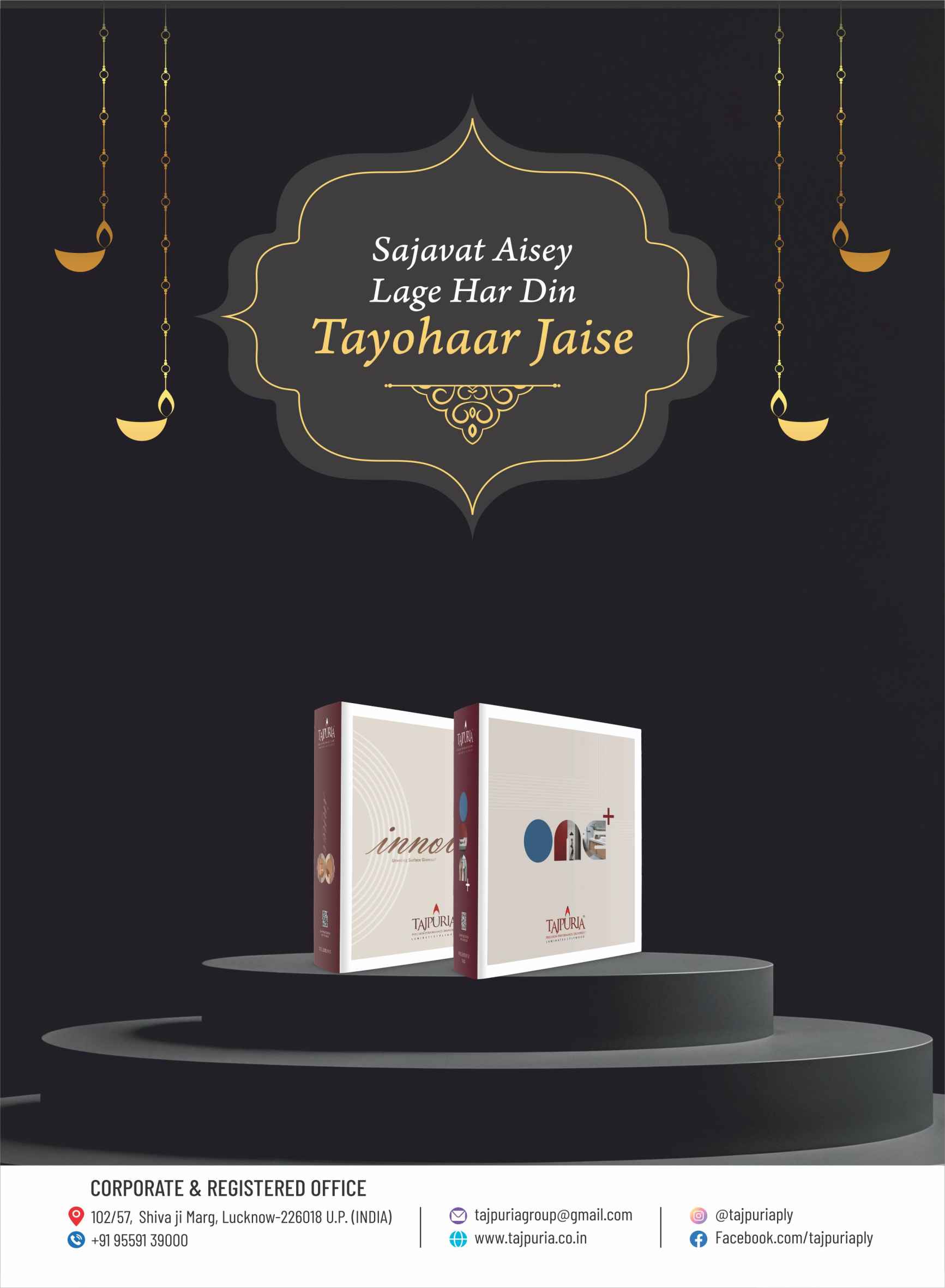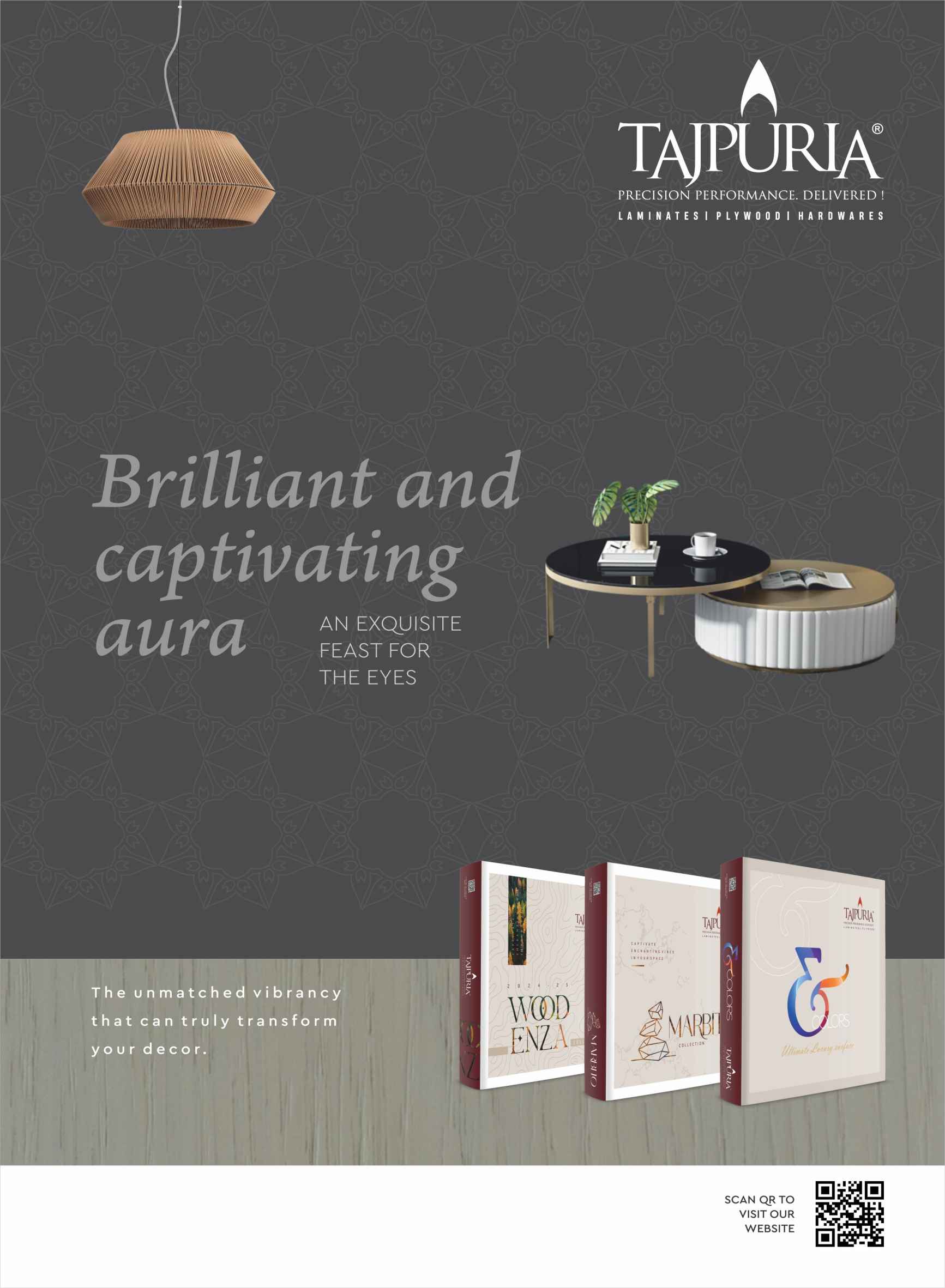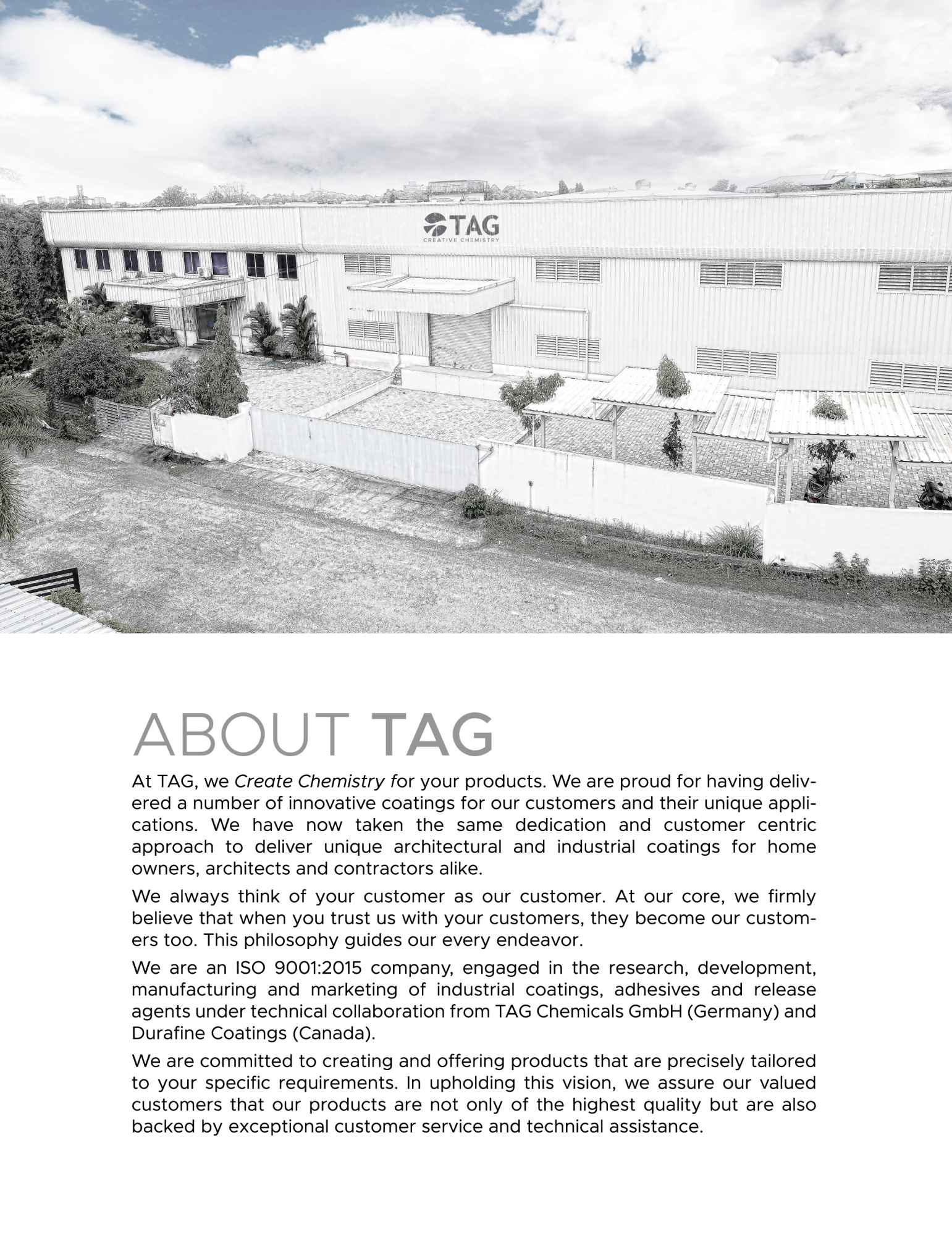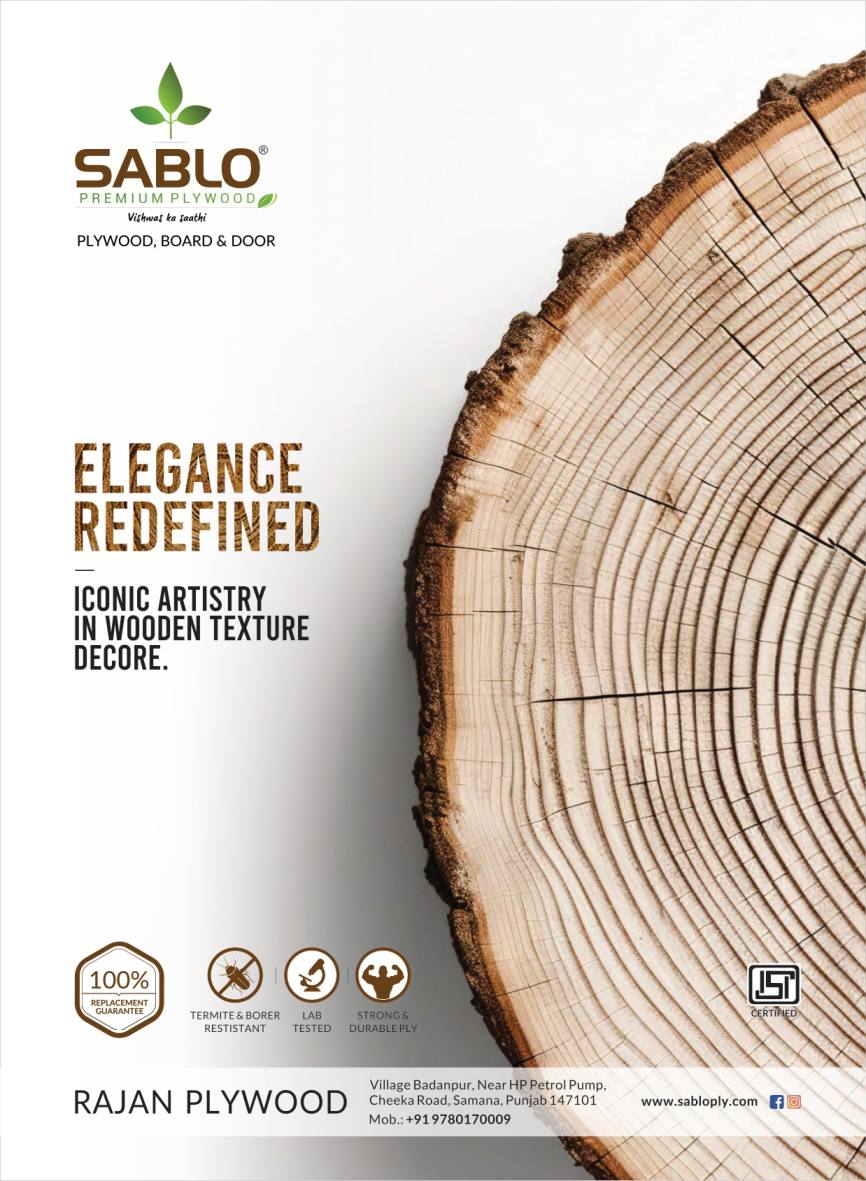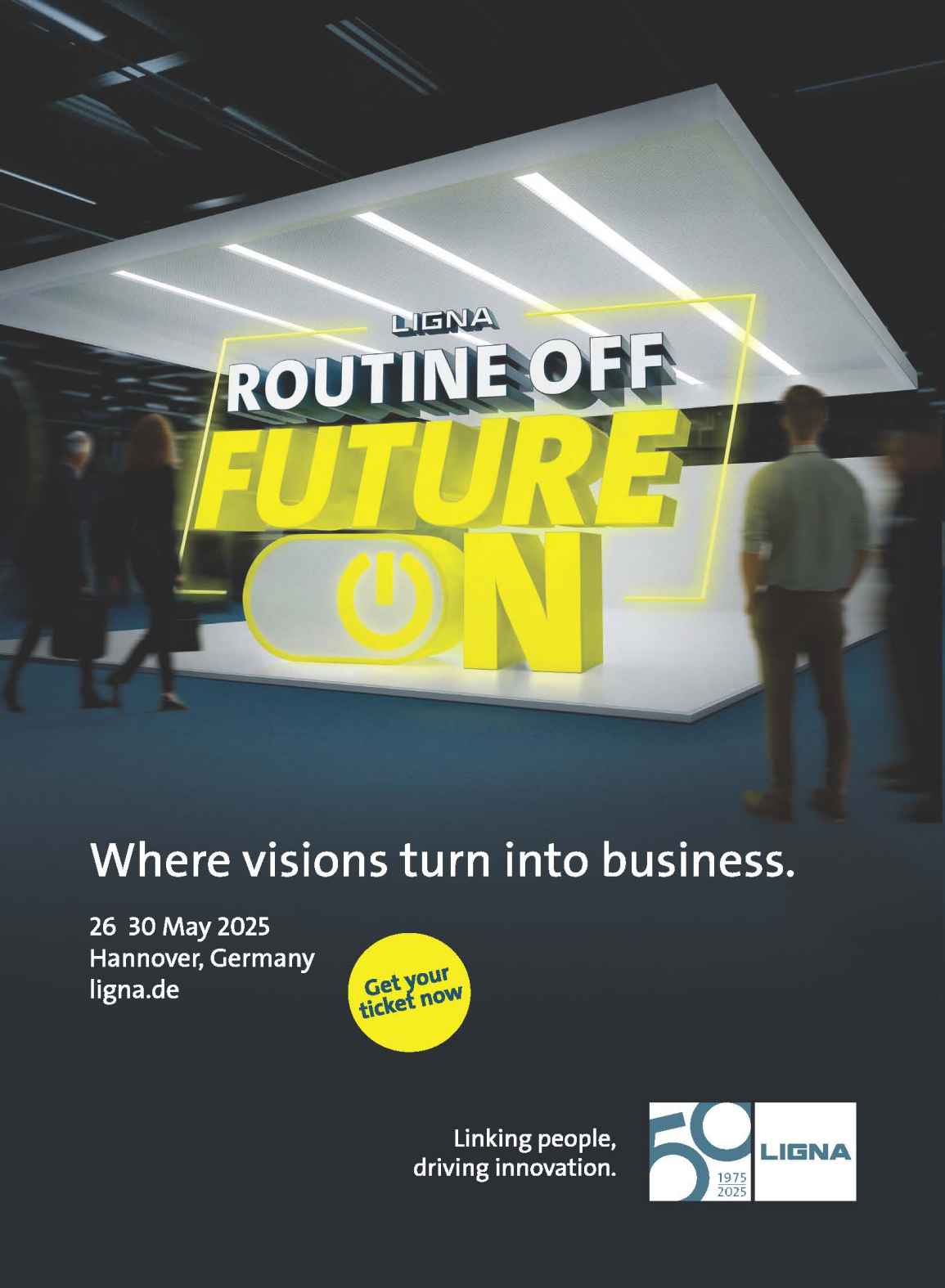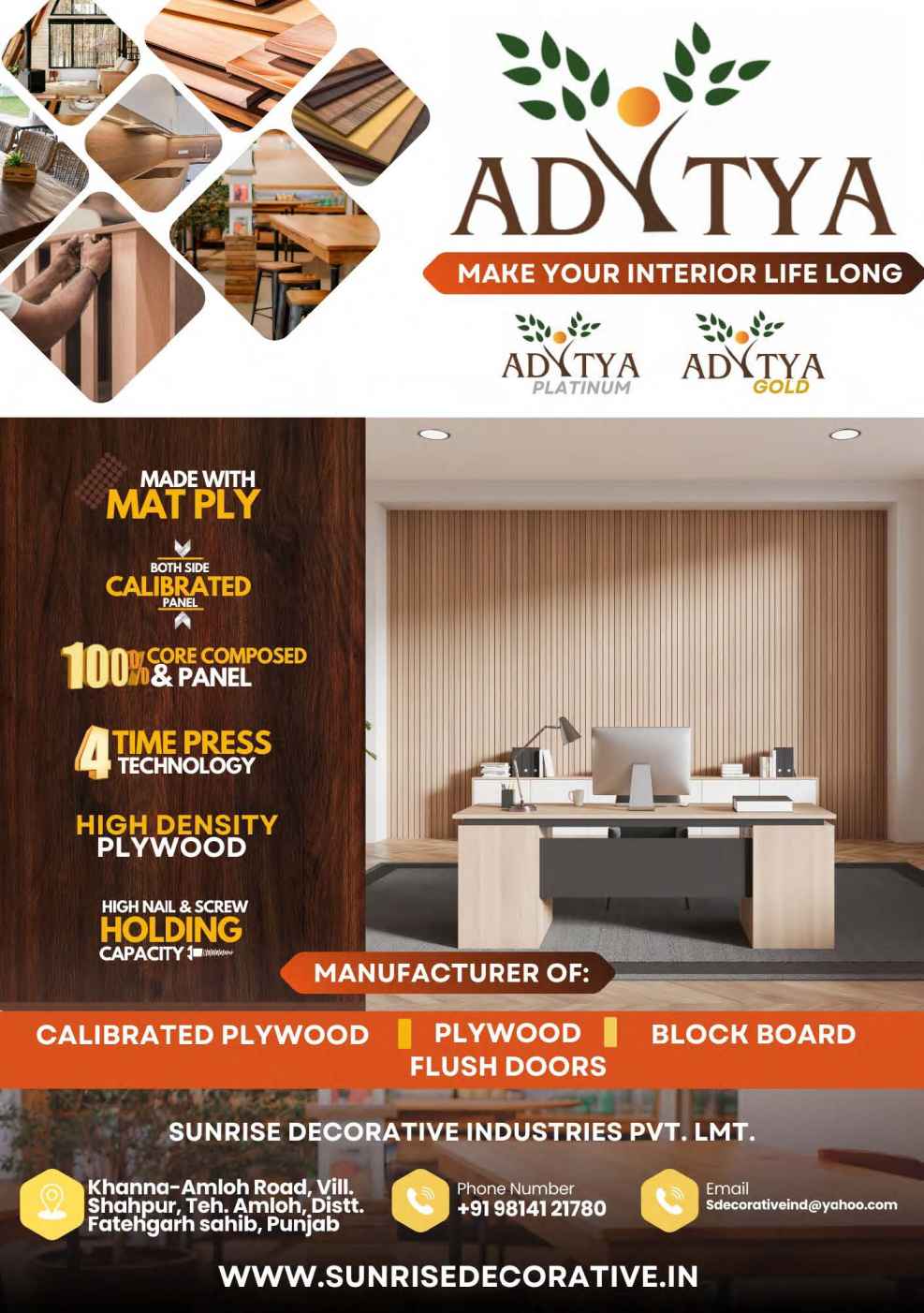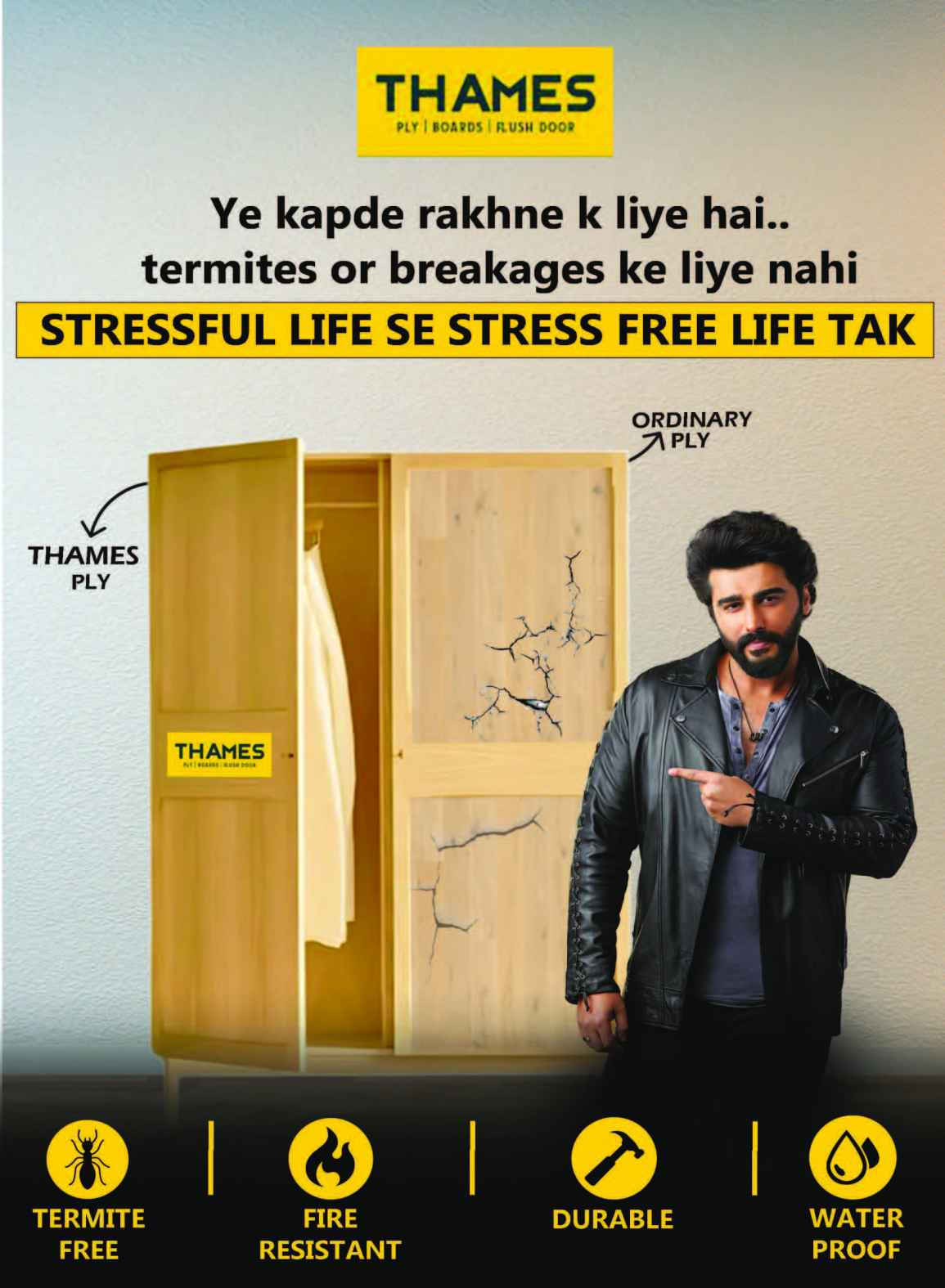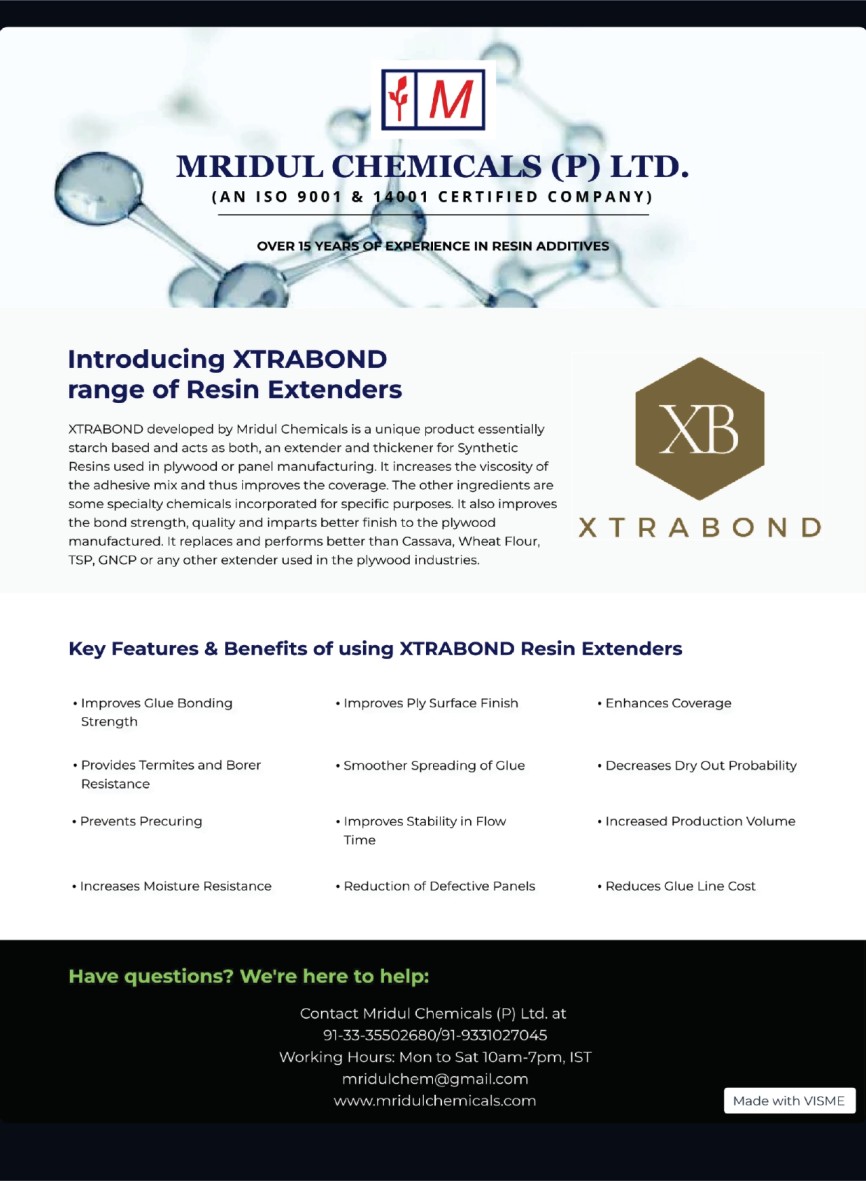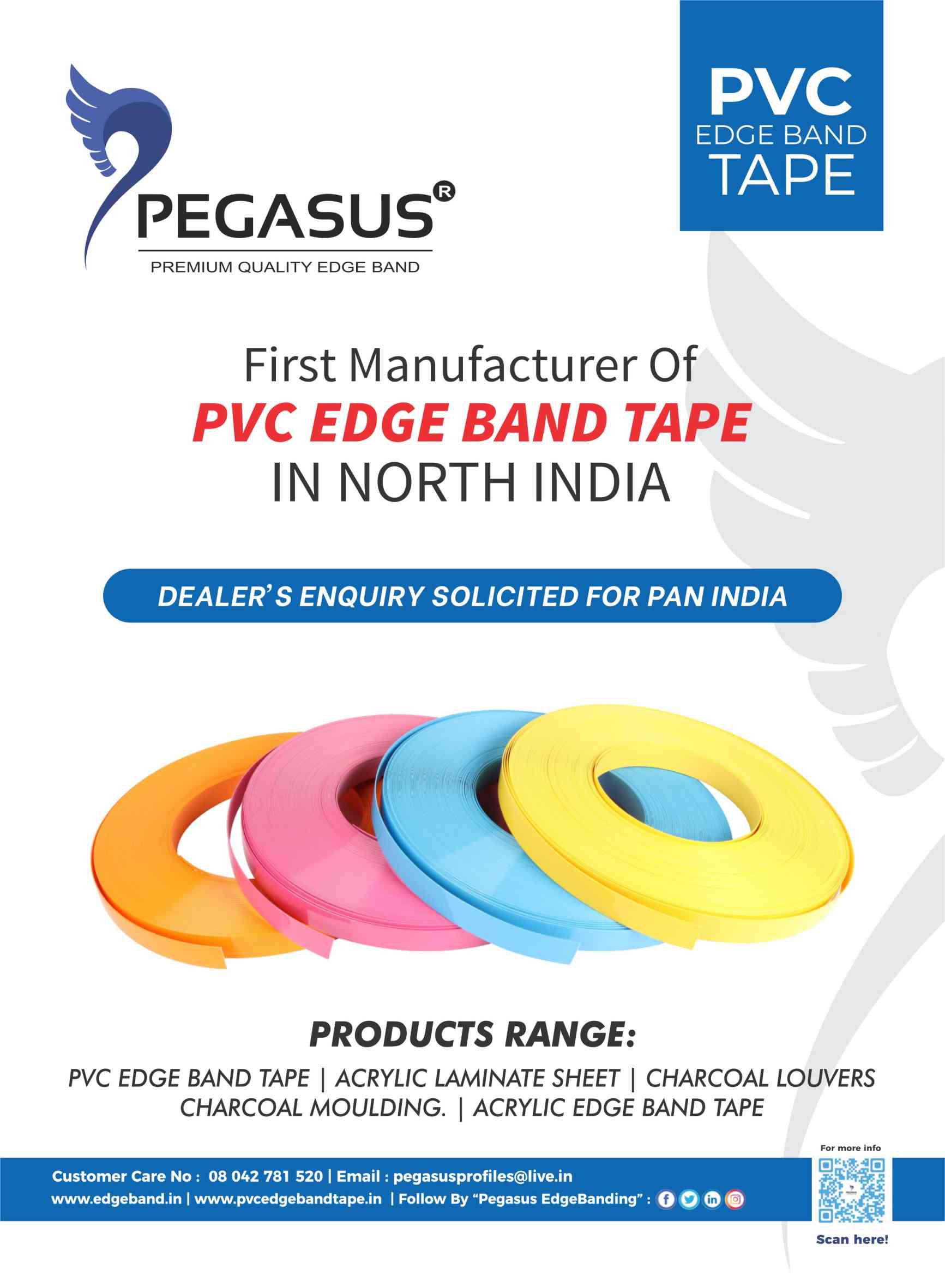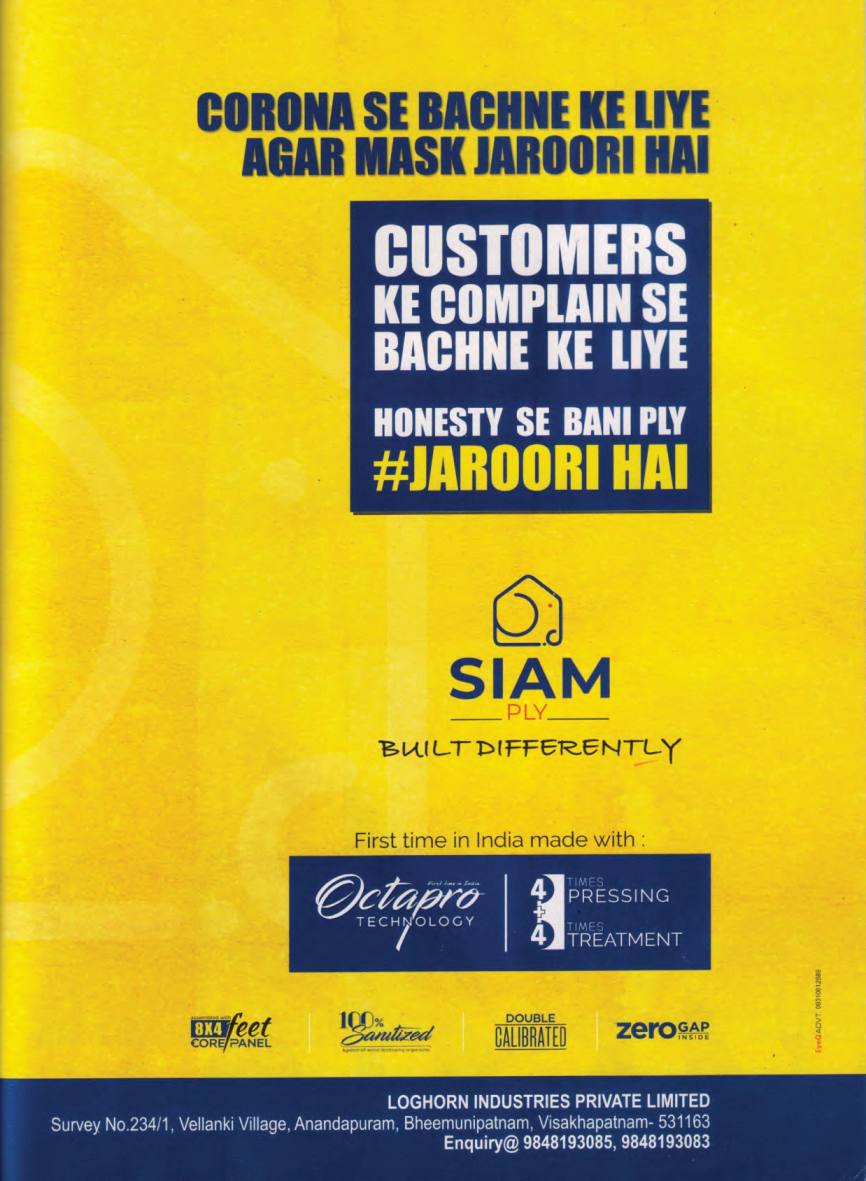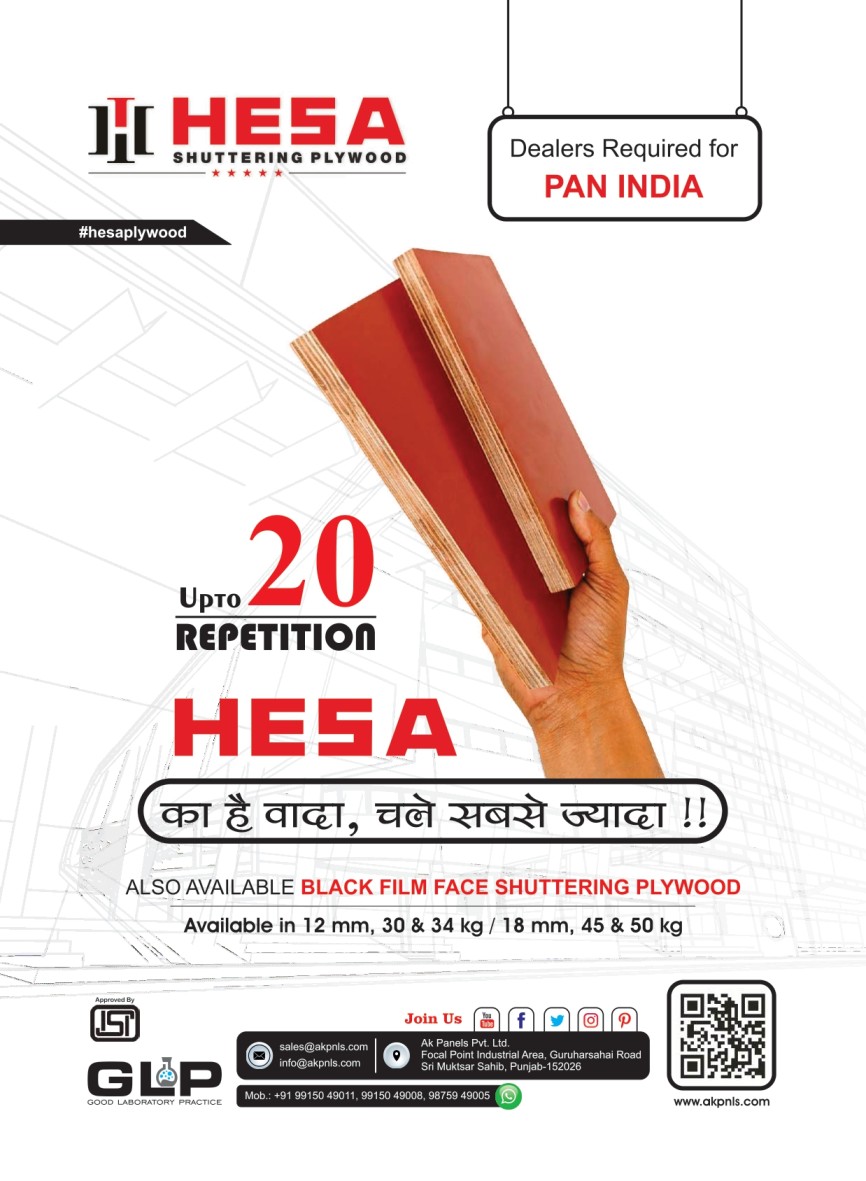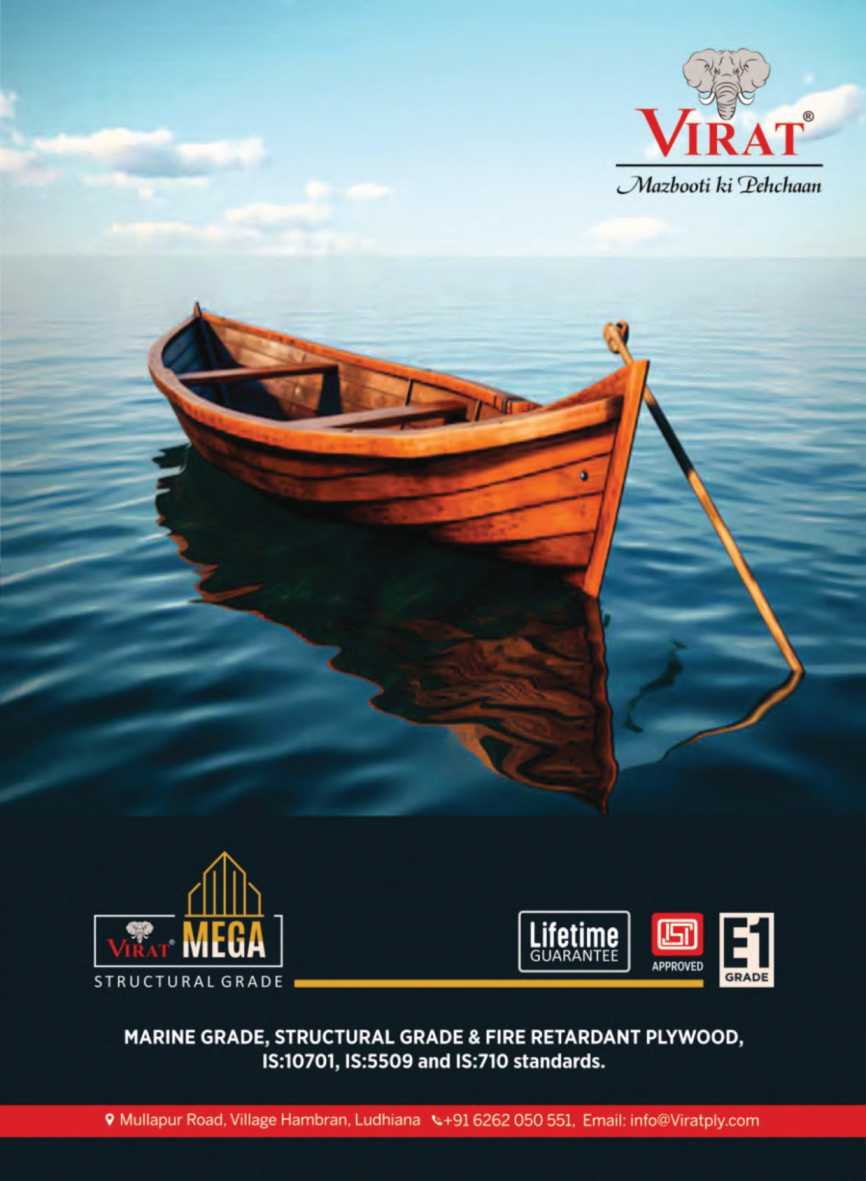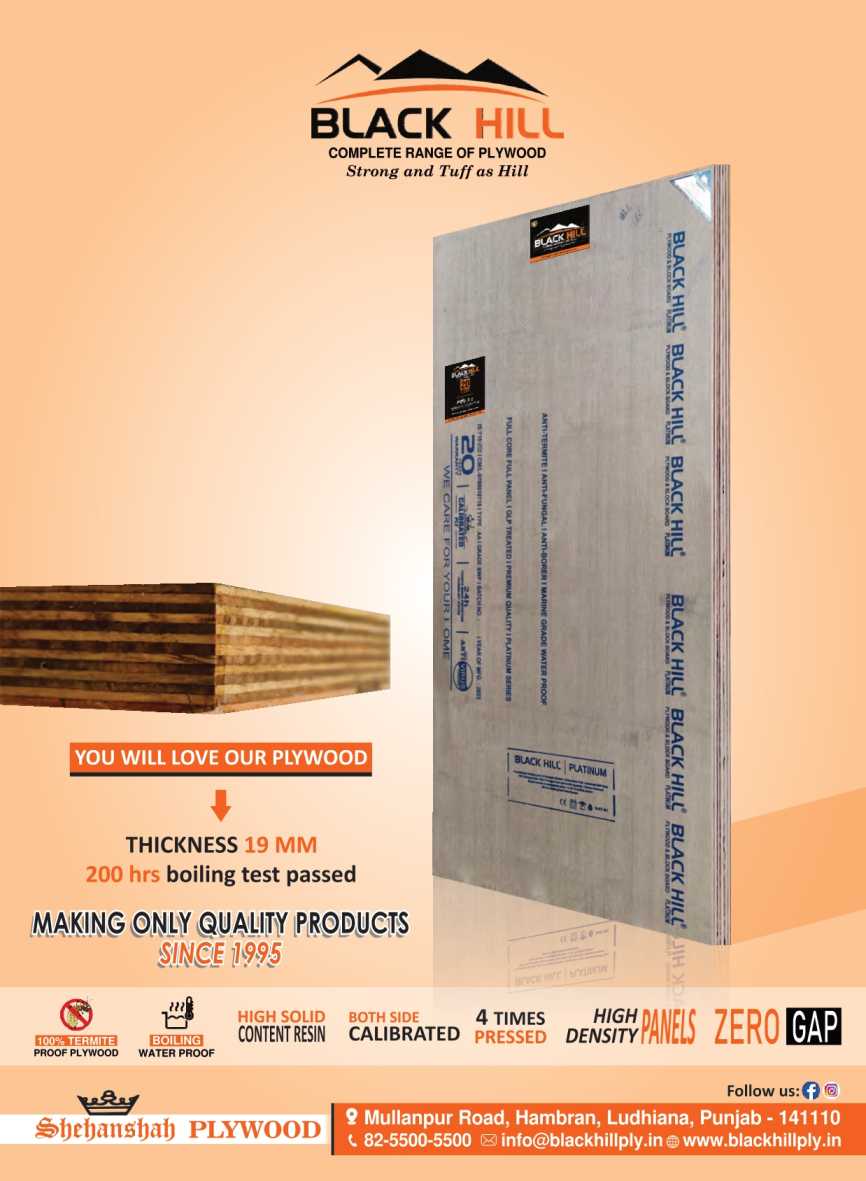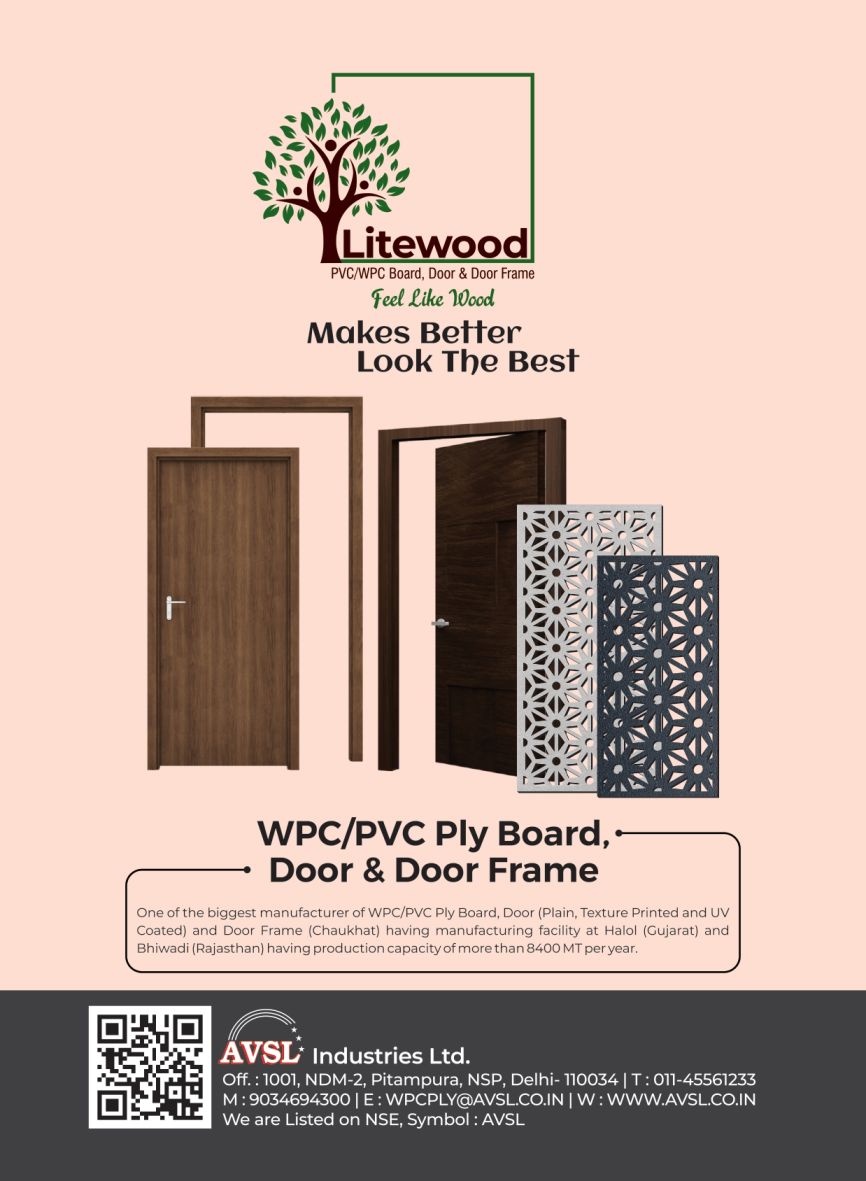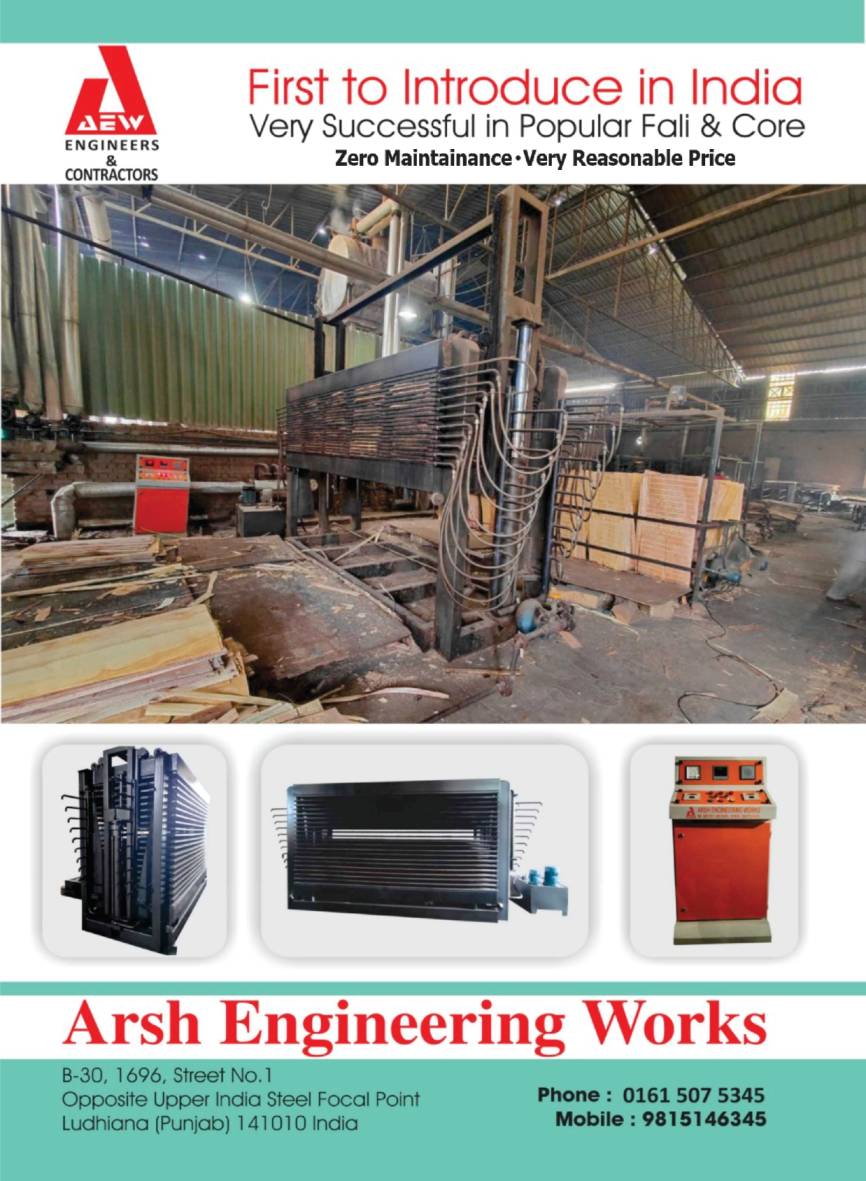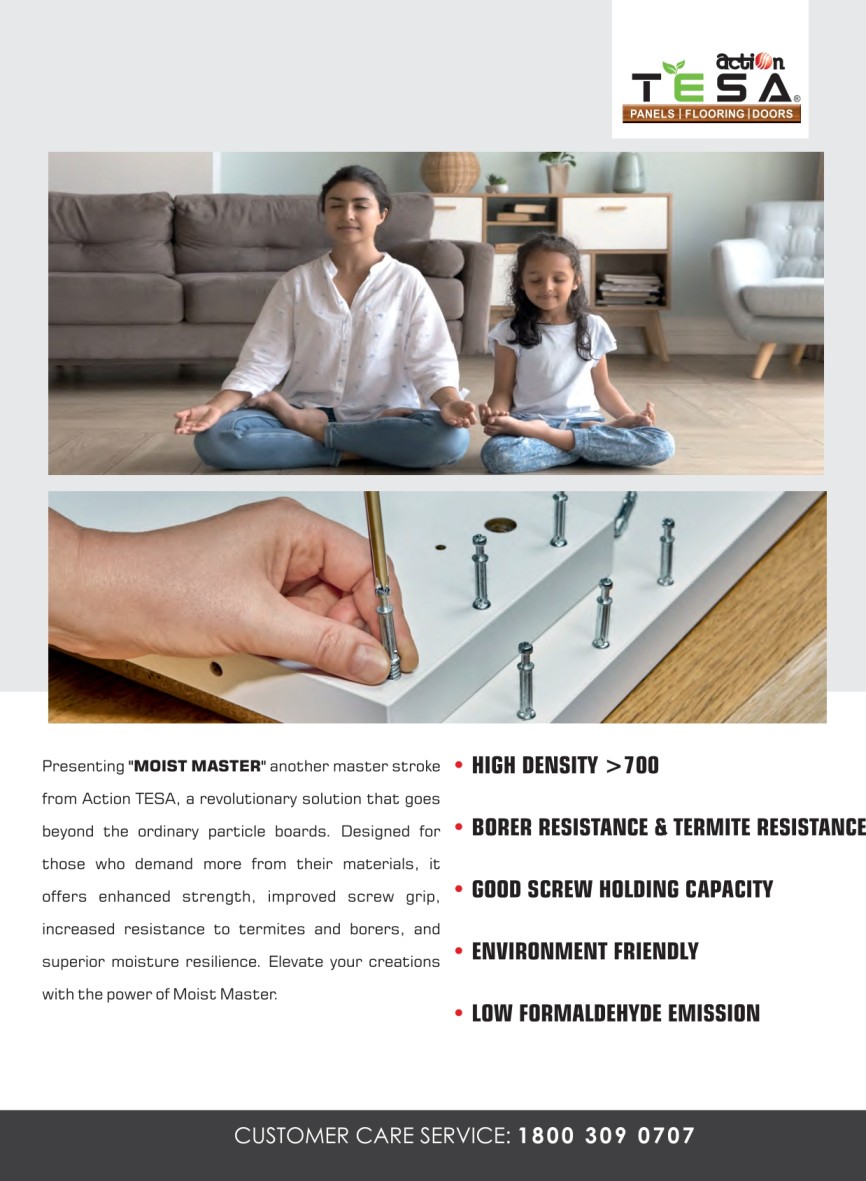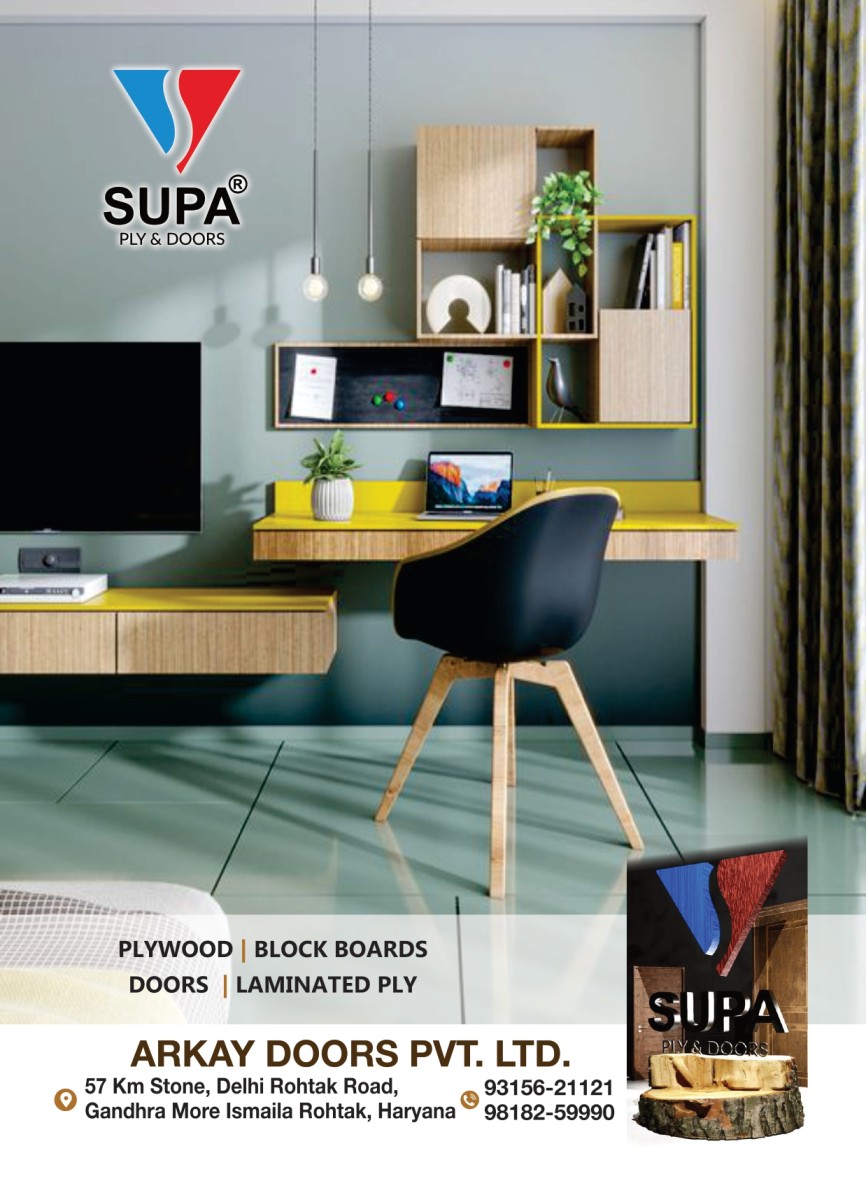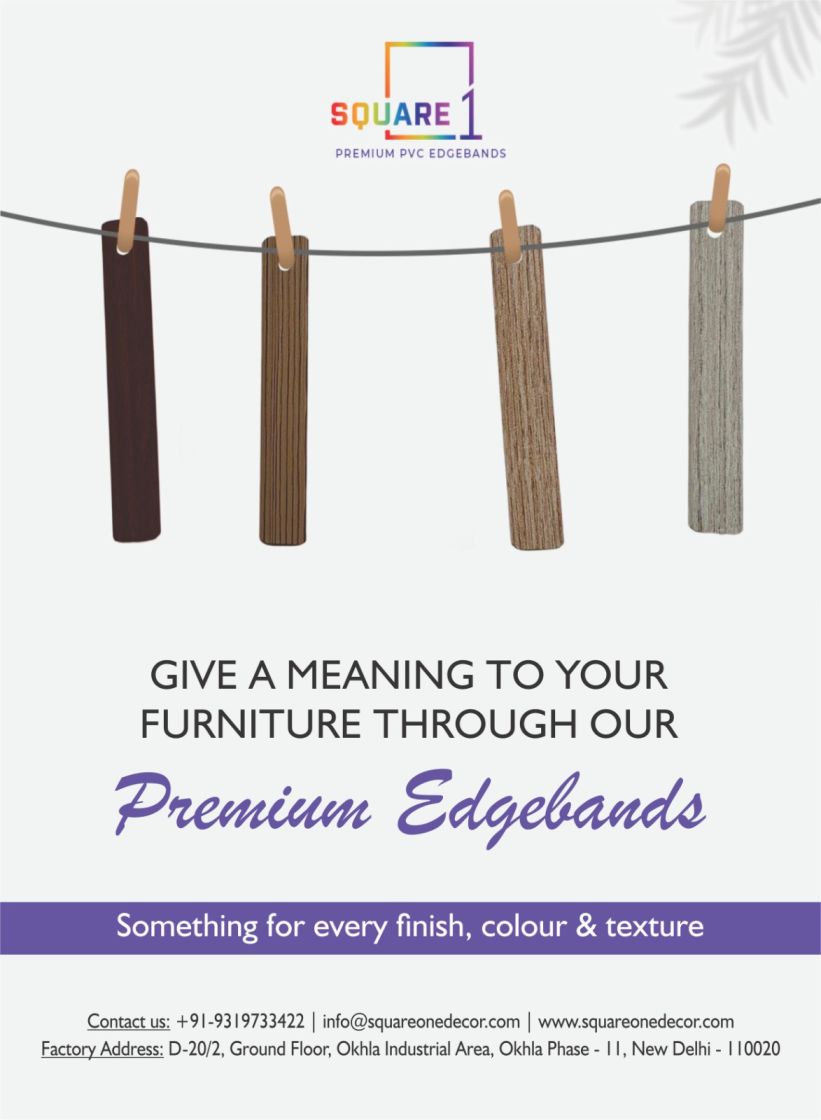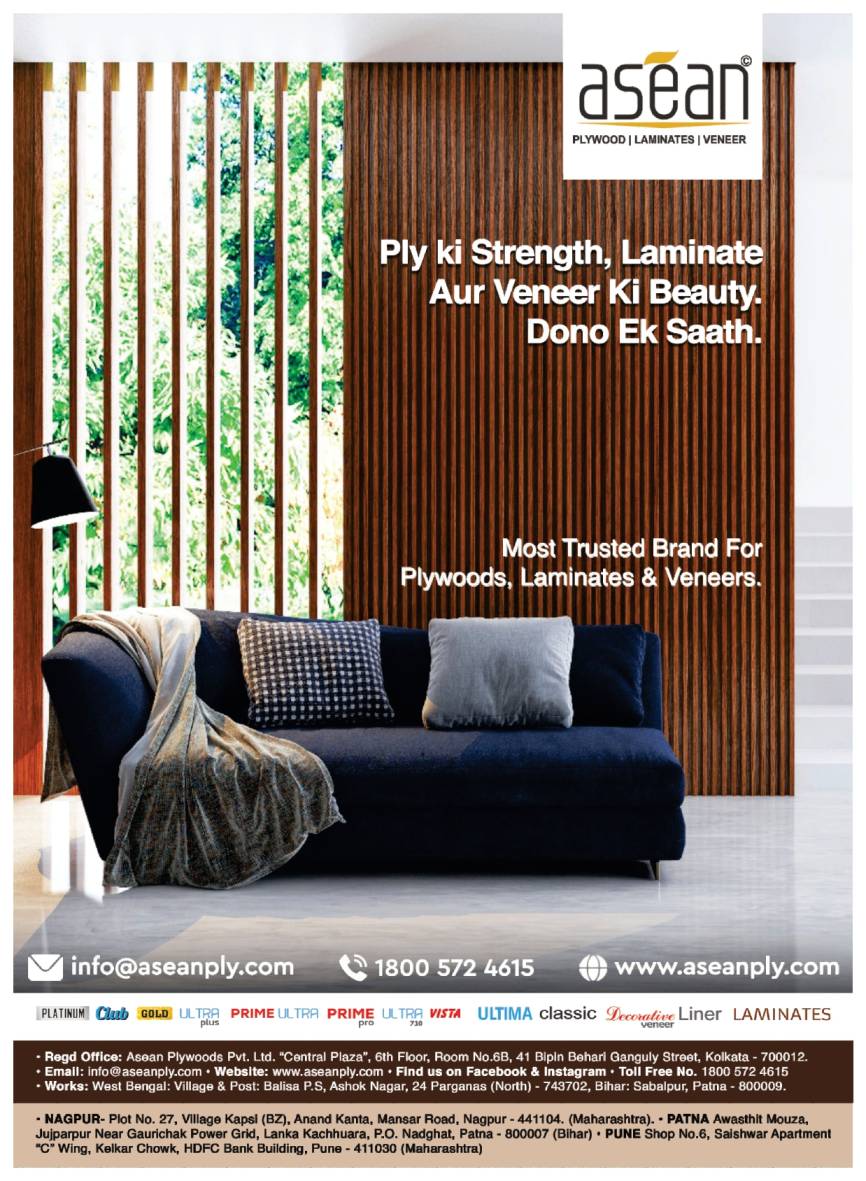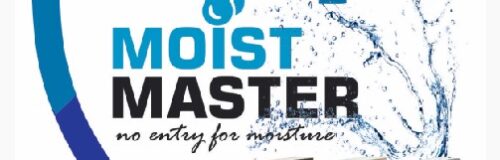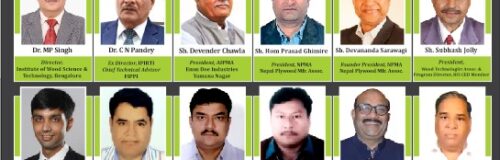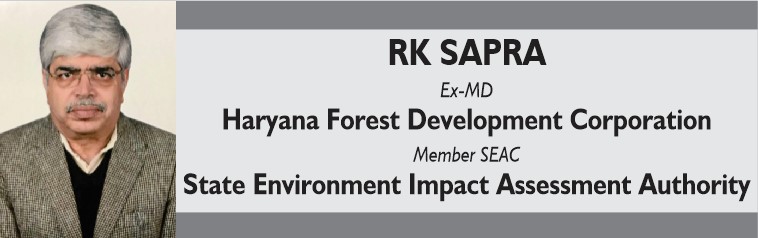
सतत् लकड़ी उत्पादन और ग्रामीण विकास के लिए अति आवश्यक लकड़ी विकास बोर्ड
- मई 10, 2025
- 0
राष्ट्रीय वन नीति (एनएफपी), 1952 मुख्य रूप से घरेलू और औद्योगिक जरूरतों को पूरा करने के लिए लकड़ी उत्पादन पर केंद्रित थी। हालांकि, एनएफपी, 1988 ने वन संरक्षण, वन प्रबंधन में स्थानीय लोगों की भागीदारी और लकड़ी आधारित उद्योगों को किसानों के साथ सीधे संबंध स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने पर जोर दिया, ताकि उनकी कच्चे माल की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। नतीजतन, लकड़ी का उत्पादन बड़े पैमाने पर निजी क्षेत्र द्वारा खेत/कृषि वानिकी के माध्यम से किया जा रहा है। कृषि वानिकी क्षेत्र लकड़ी की बढ़ती मांगों को पूरा करने, रोजगार के अवसर पैदा करने, विशेष रूप से स्कूल छोड़ने वाले युवाओं के लिए, और जलवायु संबंधी चुनौतियों के खिलाफ कृषि फसलों के लिए एक ढाल प्रदान करने सहित कई लाभ प्रदान कर रही है।
वर्तमान में, छोटी लकड़ी का उत्पादन खेतों पर लघु-चक्र वृक्ष फसलों के माध्यम से किया जाता है, जबकि बड़ी लकड़ी की मांग ज्यादातर आयात के माध्यम से पूरी की जाती है, जिसमें कुछ आपूर्ति जंगलों से होती है। 2023 में, भारत ने लकड़ी के आयात पर 2.7 बिलियन अमरीकी डॉलर खर्च किए। जिसे कम करने की सख्त जरूरत है।
हाल ही में, भारत के प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) ने ‘कृषि वानिकी‘ पर एक कार्य पत्र जारी किया, जिसमें कई साहसिक नीतिगत बदलावों की सिफारिश की गई (सान्याल एट अल., 2024)। पत्र में प्रस्ताव दिया गया है कि राज्य निजी भूमि पर सागौन, गर्जन और मेरेंटी जैसी उच्च मूल्य वाली देशी लकड़ी की प्रजातियों को कटाई और पारगमन परमिट की आवश्यकता से छूट दें। यह राष्ट्रीय पारगमन पास प्रणाली (एनटीपीएस) का विस्तार करने का भी सुझाव देता है ताकि कटाई परमिट जारी करना शामिल हो सके, इस प्रकार एकल-खिड़की निकासी प्रणाली बनाई जा सके। अंत में, पत्र में सिफारिश की गई है कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एनटीपीएस पोर्टल को अपनाएं, जिसमें किसान प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम शामिल हों। हालांकि, कुछ बाधाएं कृषि वानिकी क्षेत्र के विकास में बाधा बन रही हैं, इसके योगदान को बढ़ाने के लिए इनका समाधान किया जाना चाहिए।

लकड़ी विकास बोर्ड
2025-26 के केंद्रीय बजट में, भारत सरकार ने मखानों के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन को बढ़ावा देने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा की। बोर्ड किसानों को प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करेगा, जिससे उन्हें अपनी आय बढ़ाने के उद्देश्य से सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में मदद मिलेगी। इसी तरह के दृष्टिकोण का अनुसरण करते हुए, लकड़ी के उत्पादन को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए लकड़ी विकास बोर्ड की स्थापना आवश्यक है जो लकड़ी और लकड़ी के उत्पादों के आयात को कम करने में मदद करेगा। यह पहल राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति-2014 में सुझाई गई रणनीति के अनुसार होगी। यह पहल किसानों की आय में सुधार और रोजगार के अवसर पैदा करने में भी योगदान देगी, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में।
राज्य वन विभागों (SFD) ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के मार्गदर्शन में 1980 और 1990 के दशक के दौरान कई विदेशी सहायता प्राप्त सामाजिक वानिकी परियोजनाओं को लागू किया, जो मुख्य रूप से कृषि वानिकी पर केंद्रित थीं, जिससे लकड़ी का उत्पादन बढ़ा, किसानों की आय में वृद्धि हुई और वन और वृक्ष आवरण का विस्तार हुआ। यह देखते हुए कि कृषि वानिकी के उद्देश्य डव्म्थ्ब्ब् के अधिदेश के साथ अधिक निकटता से जुड़े हुए हैं, कृषि वानिकी की जिम्मेदारी इस मंत्रालय को हस्तांतरित करने से अधिक केंद्रित और प्रभावी कार्यान्वयन हो सकता है। दूसरा, कृषि भूमि से लकड़ी के उत्पादन को बढ़ावा देने और लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद के आयात को कम करने के लिए MoEFCC के तहत लकड़ी विकास बोर्ड की स्थापना की जा सकती है।
अनुसंधान एवं विकास पर जोर
अपनी क्षमता के बावजूद, कृषि वानिकी क्षेत्र में ऐतिहासिक रूप से अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) में अपर्याप्त निवेश हुआ है। बड़े किसान वृक्ष फसलों की खेती से अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, जबकि छोटे किसान अपनी कृषि फसलों पर न्यूनतम प्रभाव के साथ अतिरिक्त आय चाहते हैं। इसलिए, कृषि वानिकी मॉडल के विभिन्न पहलुओं में अनुसंधान एवं विकास को सभी हितधारकों की चिंताओं का समाधान ढूंढ़ना होगा।
 वन अनुसंधान संस्थान और भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (ICFRE) के तहत अन्य संस्थानों ने वाणिज्यिक वृक्ष फसलों पर मौलिक अनुसंधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। निजी कंपनियों ने वाणिज्यिक वृक्ष फसलों की उच्च उपज वाली किस्मों और क्लोनों को विकसित करके इस शोध को आगे बढ़ाया है, जिससे किसानों की गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री की मांग पूरी हो रही है। आईटीसी भद्राचलम पेपर-बोर्ड्स लिमिटेड ने देश भर में नीलगिरी, कैसुरीना और सुबाबुल की खेती को सफलतापूर्वक बढ़ावा दिया है, जबकि WIMCO ने उत्तर भारत में पोपलर की खेती को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय ने दक्षिण भारत में मेलिया डूबिया की खेती को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
वन अनुसंधान संस्थान और भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (ICFRE) के तहत अन्य संस्थानों ने वाणिज्यिक वृक्ष फसलों पर मौलिक अनुसंधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। निजी कंपनियों ने वाणिज्यिक वृक्ष फसलों की उच्च उपज वाली किस्मों और क्लोनों को विकसित करके इस शोध को आगे बढ़ाया है, जिससे किसानों की गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री की मांग पूरी हो रही है। आईटीसी भद्राचलम पेपर-बोर्ड्स लिमिटेड ने देश भर में नीलगिरी, कैसुरीना और सुबाबुल की खेती को सफलतापूर्वक बढ़ावा दिया है, जबकि WIMCO ने उत्तर भारत में पोपलर की खेती को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय ने दक्षिण भारत में मेलिया डूबिया की खेती को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
इसके अलावा, कृषि वानिकी अनुसंधान और विकास में किए गए निवेश के लिए निजी कंपनियों को कर प्रोत्साहन प्रदान किया जाना चाहिए।
विस्तार अवसंरचना को मजबूत करना
कृषि वानिकी के अंतर्गत ‘‘लैब टू लैंड‘‘ गतिविधियों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए विस्तार सुविधाओं को मजबूत करना महत्वपूर्ण है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अनुसंधान एवं विकास प्रयासों का लाभ किसानों तक पहुंचे। कृषि वानिकी के बारे में तकनीकी ज्ञान किसानों तक पहुंचाने में राज्य कृषि विभाग, कृषि विश्वविद्यालय और आईसीएआर के तहत कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, केवीके में कृषि वानिकी विशेषज्ञों के रिक्त पदों को भरने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
कृषि फसलों के साथ समानता
वर्तमान में, कृषि फसलों के लिए उपलब्ध प्रोत्साहनों को वृक्ष फसलों तक नहीं बढ़ाया गया है। जबकि कृषि फसलों की खेती करने वाले किसान किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 4-5 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण प्राप्त कर सकते हैं, वृक्ष फसलों की खेती करने वाले किसानों को बहुत अधिक दरों (14-15 प्रतिशत) पर ऋण लेना पड़ता है, जो अत्यधिक भेदभावपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, बीमा सुविधाएँ, भावांतर भारतीय योजना के तहत एमएसपी/मुआवजा, बाजार की स्थापना और कृषि फसलों के लिए उपलब्ध ई-एनएएम प्लेटफॉर्म को वृक्ष फसलों तक नहीं बढ़ाया गया है। चूंकि कई राज्यों ने कृषि उपज के रूप में खेत की लकड़ी को घोषित किया है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि कृषि फसलों को दिए जाने वाले सभी प्रोत्साहन वृक्ष फसलों तक बढ़ाए जाएं।

आगे की राह
‘कृषि वानिकी‘ पर ईएसी-पीएम के कार्य पत्र में की गई सिफारिशें भारत के आर्थिक विकास में इस क्षेत्र की अधिक पहचान को सुगम बना सकती हैं। ये अंतर्दृष्टि नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं, विशेष रूप से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (एमओएएफडब्ल्यू) की पूरक भूमिकाओं को स्पष्ट करने में, जो कृषि भूमि से लकड़ी के उत्पादन को बढ़ाने में सहायक हैं।
इसके अलावा, ईएसी-पीएम प्रस्तावित लकड़ी विकास बोर्ड के लिए वित्तीय आवंटन में वृद्धि की वकालत कर सकता है, साथ ही कॉर्पारेट क्षेत्र के लिए विस्तारित भूमिका की वकालत कर सकता है, जिसने अतीत में मजबूत प्रदर्शन का प्रदर्शन किया है।
अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल को मजबूत करना आवश्यक होगा। इन नीतिगत प्रस्तावों से इससे क्षेत्र के प्रदर्शन को बढ़ावा मिलने और ग्रामीण क्षेत्रों को महत्वपूर्ण लाभ मिलने की उम्मीद है, जो शहरी क्षेत्रों में सीमित रोजगार के अवसरों के कारण रिवर्स माइग्रेशन से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं।